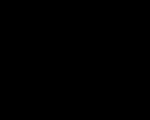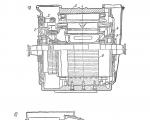प्रकृति में ऊर्जा का प्रवाह. प्रकृति में पदार्थ और ऊर्जा का चक्र
किसी भी जीवन को ऊर्जा और पदार्थ के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है। ऊर्जा बुनियादी जीवन प्रतिक्रियाओं को पूरा करने में खर्च की जाती है, पदार्थ का उपयोग जीवों के शरीर के निर्माण के लिए किया जाता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का अस्तित्व जीवित और निर्जीव प्रकृति के बीच सामग्री और ऊर्जा विनिमय की जटिल प्रक्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ है। ये प्रक्रियाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं और न केवल जैविक समुदायों की संरचना पर, बल्कि उनके भौतिक पर्यावरण पर भी निर्भर करती हैं।
समुदाय में ऊर्जा का प्रवाह– यह कार्बनिक यौगिकों (भोजन) के रासायनिक बंधों के रूप में एक स्तर के जीवों से दूसरे स्तर तक इसका संक्रमण है।
पदार्थ का प्रवाह (चक्र) रासायनिक तत्वों और उनके यौगिकों के रूप में उत्पादकों से अपघटकों तक और फिर (जीवित जीवों की भागीदारी के बिना होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से) उत्पादकों तक पदार्थ की गति है।
पदार्थ का संचलन और ऊर्जा का प्रवाह समान अवधारणाएं नहीं हैं, हालांकि विभिन्न ऊर्जा समकक्षों (कैलोरी, किलोकैलोरी, जूल) का उपयोग अक्सर पदार्थ की गति को मापने के लिए किया जाता है। यह आंशिक रूप से इस तथ्य से समझाया गया है कि सभी ट्रॉफिक स्तरों पर, पहले को छोड़कर, जीवों के जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा को उपभोग किए गए भोजन के पदार्थ के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। केवल पौधे (उत्पादक) ही अपनी जीवन गतिविधि के लिए सूर्य की उज्ज्वल ऊर्जा का सीधे उपयोग कर सकते हैं।
किसी पारिस्थितिकी तंत्र में घूमने वाले पदार्थ का एक सख्त माप व्यक्तिगत रासायनिक तत्वों के परिसंचरण को ध्यान में रखकर प्राप्त किया जा सकता है, मुख्य रूप से वे जो पौधे और पशु कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के लिए मुख्य निर्माण सामग्री हैं।
उन पदार्थों के विपरीत जो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न ब्लॉकों के माध्यम से लगातार घूमते रहते हैं और हमेशा चक्र में फिर से प्रवेश कर सकते हैं, ऊर्जा का उपयोग शरीर में केवल एक बार किया जा सकता है।
भौतिकी के नियमों के अनुसार, ऊर्जा एक रूप (जैसे प्रकाश ऊर्जा) से दूसरे रूप (जैसे भोजन की संभावित ऊर्जा) में बदल सकती है, लेकिन यह कभी भी दोबारा निर्मित या नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा के परिवर्तन से जुड़ी एक भी प्रक्रिया इसका कुछ हिस्सा खोए बिना नहीं हो सकती। इसके परिवर्तनों में, ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है और इसलिए नष्ट हो जाती है। इस कारण से, उदाहरण के लिए, खाद्य पदार्थों का जीव के शरीर को बनाने वाले पदार्थों में परिवर्तन नहीं हो सकता है, जो एक सौ प्रतिशत दक्षता के साथ होता है।
सभी पारिस्थितिक तंत्रों का अस्तित्व ऊर्जा के निरंतर प्रवाह पर निर्भर करता है, जो सभी जीवों के लिए उनके महत्वपूर्ण कार्यों और आत्म-प्रजनन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
हरे पौधों पर पड़ने वाले सौर प्रवाह का लगभग आधा हिस्सा ही प्रकाश संश्लेषक तत्वों द्वारा अवशोषित किया जाता है, और अवशोषित ऊर्जा का केवल एक छोटा सा अंश (1/100 से 1/20 भाग तक) गतिविधि के लिए आवश्यक ऊर्जा के रूप में संग्रहीत होता है पौधे के ऊतकों का.
जैसे-जैसे कोई प्राथमिक उत्पादक से दूर जाता है, ऊर्जा प्रवाह की दर (अर्थात, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा इकाइयों में व्यक्त ऊर्जा की मात्रा) तेजी से कम हो जाती है।
एक पोषी स्तर से उच्चतर पोषी स्तर तक संक्रमण के दौरान ऊर्जा की मात्रा में गिरावट इन स्तरों की संख्या स्वयं निर्धारित करती है। यह अनुमान लगाया गया है कि किसी भी पोषी स्तर को पिछले स्तर की ऊर्जा का लगभग 10% (या थोड़ा अधिक) ही प्राप्त होता है। इसलिए, पोषी स्तरों की कुल संख्या शायद ही कभी 3-4 से अधिक हो।
विभिन्न पोषी स्तरों पर जीवित पदार्थ का अनुपात आम तौर पर आने वाली ऊर्जा के अनुपात के समान नियम का पालन करता है: स्तर जितना अधिक होगा, कुल बायोमास और उसके घटक जीवों की संख्या उतनी ही कम होगी।
जीवों के विभिन्न समूहों की संख्या का अनुपात समुदाय की स्थिरता का अंदाजा देता है, क्योंकि बायोमास और कुछ आबादी की संख्या एक ही समय में इस और अन्य प्रजातियों के जीवों के लिए रहने की जगह का संकेतक है . उदाहरण के लिए, किसी जंगल में पेड़ों की संख्या न केवल उनमें मौजूद बायोमास और ऊर्जा की कुल आपूर्ति निर्धारित करती है, बल्कि माइक्रॉक्लाइमेट, साथ ही कई कीड़ों और पक्षियों के लिए आश्रयों की संख्या भी निर्धारित करती है।
संख्याओं के पिरामिडों को उलटा किया जा सकता है। ऐसा तब होता है जब शिकार की आबादी की प्रजनन दर अधिक होती है, और यहां तक कि कम बायोमास पर भी, ऐसी आबादी उन शिकारियों के लिए पर्याप्त भोजन स्रोत हो सकती है जिनके पास उच्च बायोमास है लेकिन प्रजनन दर कम है। उदाहरण के लिए, कई कीड़े एक पेड़ (एक उलटा जनसंख्या पिरामिड) पर रह सकते हैं और भोजन कर सकते हैं। बायोमास का उलटा पिरामिड जलीय पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है, जहां प्राथमिक उत्पादक (फाइटोप्लांकटोनिक शैवाल) बहुत तेजी से विभाजित होते हैं और संख्या में गुणा करते हैं, और उनके उपभोक्ता (ज़ूप्लैंकटोनिक क्रस्टेशियंस) बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनका प्रजनन चक्र लंबा होता है।
चरागाह और डेट्राइटल श्रृंखलाएं
किसी समुदाय में ऊर्जा कई अलग-अलग तरीकों से प्रवाहित हो सकती है। यह सभी उपभोक्ताओं की खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है(उपभोक्ता प्रणाली) दो और लिंक जोड़ने के साथ: यह मृत कार्बनिक पदार्थऔर विघटक खाद्य शृंखला(घटाने वाली प्रणाली)।
पौधों से शाकाहारी जीवों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह(उन्हें चराई कहा जाता है), चरागाह खाद्य शृंखला कहलाती है।
जिन जीवों का वे उपभोग करते हैं उनके अवशेष जो उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग नहीं किए जाते हैं वे मृत कार्बनिक पदार्थों की भरपाई करते हैं। इसमें मल शामिल होता है जिसमें अपाच्य भोजन का हिस्सा, साथ ही जानवरों की लाशें, वनस्पति अवशेष (पत्तियां, शाखाएं, शैवाल) शामिल होते हैं और इसे कहा जाता है डिटरिटस
मृत कार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न होने वाली और विघटित प्रणाली से गुजरने वाली ऊर्जा के प्रवाह को डेट्राइटल खाद्य श्रृंखला कहा जाता है।
समानताओं के साथ-साथ, चरागाह और डेट्राइटल खाद्य श्रृंखलाओं की कार्यप्रणाली में गहरा अंतर भी है। यह इस तथ्य में निहित है कि में उपभोक्ता प्रणाली में, मल और मृत जीव नष्ट हो जाते हैं, और रिडक्टिव प्रणाली में– नहीं।
देर-सबेर, मृत कार्बनिक पदार्थ में निहित ऊर्जा पूरी तरह से डीकंपोजर द्वारा उपयोग की जाएगी और श्वसन के माध्यम से गर्मी के रूप में नष्ट हो जाएगी, भले ही इसके लिए कई बार डीकंपोजर की प्रणाली से गुजरने की आवश्यकता हो।एकमात्र अपवाद वे मामले हैं जब स्थानीय अजैविक परिस्थितियाँ अपघटन प्रक्रिया (उच्च आर्द्रता, पर्माफ्रॉस्ट) के लिए बहुत प्रतिकूल होती हैं। इन मामलों में, अपूर्ण रूप से संसाधित, अत्यधिक ऊर्जा-गहन पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है, जो समय के साथ और उपयुक्त परिस्थितियों में दहनशील कार्बनिक जीवाश्मों - तेल, कोयला, पीट में बदल जाते हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का चक्र
प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता विशेष रूप से तब स्पष्ट रूप से प्रकट होती है जब उनमें घूमने वाले पदार्थ के प्रवाह पर विचार किया जाता है। पदार्थ को बंद चक्रों (परिसंचरण) में प्रसारित किया जा सकता है, जो जीवों और पर्यावरण के बीच बार-बार प्रसारित होता है।
रासायनिक तत्वों (अर्थात पदार्थों) की वृत्ताकार गति (भूमि, वायु, जल के माध्यम से) को जैव-भू-रासायनिक चक्र या परिसंचरण कहा जाता है।
जीवन के लिए आवश्यक तत्वों एवं घुले हुए लवणों को परंपरागत रूप से कहा जाता है पोषक तत्व(जीवन देना) या पोषक तत्व।बायोजेनिक तत्वों के बीच, दो समूह प्रतिष्ठित हैं: मैक्रोट्रॉफिक पदार्थ और माइक्रोट्रॉफिक पदार्थ।
मैक्रोट्रॉफ़िक पदार्थउन तत्वों को कवर करें जो जीवित जीवों के ऊतकों का रासायनिक आधार बनाते हैं। इनमें शामिल हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर।
सूक्ष्मपोषी पदार्थइसमें तत्व और उनके यौगिक शामिल हैं, जो जीवित प्रणालियों के अस्तित्व के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ऐसे पदार्थों को अक्सर कहा जाता है सूक्ष्म तत्वये हैं लोहा, मैंगनीज, तांबा, जस्ता, बोरान, सोडियम, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, वैनेडियम और कोबाल्ट। हालाँकि सूक्ष्मपोषी तत्व बहुत कम मात्रा में जीवों के लिए आवश्यक हैं, लेकिन उनकी कमी उत्पादकता को गंभीर रूप से सीमित कर सकती है।
पोषक तत्वों का संचलन आमतौर पर उनके रासायनिक परिवर्तनों के साथ होता है। उदाहरण के लिए, नाइट्रेट नाइट्रोजन को प्रोटीन नाइट्रोजन में परिवर्तित किया जा सकता है, फिर यूरिया में परिवर्तित किया जा सकता है, अमोनिया में परिवर्तित किया जा सकता है और सूक्ष्मजीवों के प्रभाव में फिर से नाइट्रेट रूप में संश्लेषित किया जा सकता है। विभिन्न तंत्र, जैविक और रासायनिक दोनों, विनाइट्रीकरण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं।
पोषक तत्वों का भंडार परिवर्तनशील है। उनमें से कुछ को जीवित बायोमास के रूप में अलग करने की प्रक्रिया से अजैविक वातावरण में शेष मात्रा कम हो जाती है। और यदि पौधे और अन्य जीव अंततः विघटित नहीं हुए, तो पोषक तत्वों की आपूर्ति समाप्त हो जाएगी और पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं हेटरोट्रॉफ़्स की गतिविधि, मुख्य रूप से डेट्राइटल श्रृंखलाओं में कार्य करने वाले जीव,– पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने और उत्पादों के निर्माण में एक निर्णायक कारक।
आइए कुछ संख्यात्मक आंकड़ों पर नजर डालें जो जैव-भू-रासायनिक कार्बन चक्र की ओर मुड़ते हुए पदार्थ स्थानांतरण के पैमाने को दर्शाते हैं। पौधों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले कार्बन का प्राकृतिक स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वायुमंडल का हिस्सा है या पानी में घुल जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड (कार्बन डाइऑक्साइड) कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है जो जानवरों के लिए भोजन के रूप में कार्य करता है। श्वसन, किण्वन और ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में लौट आती है।
हमारे ग्रह के वायुमंडल में कार्बन भंडार 700 अरब टन, जलमंडल में - 50,000 अरब टन होने का अनुमान है। वार्षिक गणना के अनुसार, प्रकाश संश्लेषण के परिणामस्वरूप, भूमि और पानी में पौधों के द्रव्यमान में वृद्धि 30 अरब टन है और क्रमशः 150 अरब टन, कार्बन चक्र लगभग 300 वर्षों तक चलता रहता है।
दूसरा उदाहरण फॉस्फोरस चक्र है। फॉस्फोरस के मुख्य भंडार में विभिन्न चट्टानें होती हैं, जो धीरे-धीरे (विनाश और क्षरण के परिणामस्वरूप) अपने फॉस्फेट को स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में छोड़ती हैं। फॉस्फेट पौधों द्वारा उपभोग किए जाते हैं और कार्बनिक पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जब जानवरों के शवों को सूक्ष्मजीवों द्वारा विघटित किया जाता है, तो फॉस्फेट मिट्टी में वापस आ जाते हैं और फिर पौधों द्वारा फिर से उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा, फॉस्फेट का कुछ हिस्सा जलधाराओं द्वारा समुद्र में ले जाया जाता है। यह फाइटोप्लांकटन और उस पर निर्भर सभी खाद्य श्रृंखलाओं के विकास को सुनिश्चित करता है। समुद्री जल में मौजूद फास्फोरस का कुछ भाग गुआनो के रूप में भूमि पर वापस आ सकता है।
पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल ऊर्जा चक्र
परिचय
पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा और संरचना
1 पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा
2 पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण
3 मैक्रोइकोसिस्टम की ज़ोनिंग
4 पारिस्थितिकी तंत्र संरचना
कारक जो पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता सुनिश्चित करते हैं
1 पदार्थ चक्र
2 पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह
3 गतिशील प्रक्रियाएं जो पारिस्थितिक तंत्र में अखंडता और स्थिरता सुनिश्चित करती हैं
4 एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जीवमंडल जो पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता और स्थिरता सुनिश्चित करता है
निष्कर्ष
परिचय
पारिस्थितिकी तंत्र जीवों और अकार्बनिक घटकों का कोई संग्रह है जिसमें पदार्थों का संचलन हो सकता है। एन.एफ. के अनुसार रीमर्स (1990), एक पारिस्थितिकी तंत्र जीवित प्राणियों और उसके आवास का कोई भी समुदाय है, जो एक एकल कार्यात्मक संपूर्ण में एकजुट होता है, जो व्यक्तिगत पर्यावरणीय घटकों के बीच मौजूद अन्योन्याश्रय और कारण-और-प्रभाव संबंधों के आधार पर उत्पन्न होता है। ए. टैन्सले (1935) ने निम्नलिखित संबंध प्रस्तावित किया:
माइक्रोइकोसिस्टम, मेसोइकोसिस्टम, मैक्रोइकोसिस्टम और वैश्विक जीवमंडल हैं। बड़े स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बायोम कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र अव्यवस्था में बिखरे हुए नहीं हैं; इसके विपरीत, वे क्षैतिज (अक्षांश में) और लंबवत (ऊंचाई में) दोनों, काफी नियमित क्षेत्रों में समूहीकृत हैं।
भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक, विभिन्न गोलार्धों के बायोम के वितरण में एक निश्चित समरूपता दिखाई देती है: उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, रेगिस्तान, मैदान, समशीतोष्ण वन, शंकुधारी वन, टैगा।
प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक होते हैं: जीव और उनके निर्जीव पर्यावरण के कारक। जीवों (पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव) की समग्रता को पारिस्थितिकी तंत्र का बायोटा कहा जाता है। पोषी संरचना (ग्रीक ट्रॉफ - पोषण से) के दृष्टिकोण से, पारिस्थितिकी तंत्र को दो स्तरों में विभाजित किया जा सकता है: ऊपरी, निचला।
निम्नलिखित घटकों को एक पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है: अकार्बनिक, कार्बनिक यौगिक, वायु, पानी और सब्सट्रेट वातावरण, उत्पादक, स्वपोषी जीव, उपभोक्ता, या फागोट्रोफ, डीकंपोजर और डिट्रिटिवोर्स।
पृथ्वी पर सौर ऊर्जा पदार्थों के दो चक्रों का कारण बनती है: बड़े, या भूवैज्ञानिक, और छोटे, जैविक (जैविक)।
पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का चक्र होता है। सबसे अधिक अध्ययन किए गए हैं: कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आदि के चक्र।
जीवों की महत्वपूर्ण गतिविधि का रखरखाव और पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थ का संचलन, यानी पारिस्थितिक तंत्र का अस्तित्व, सौर ऊर्जा के निरंतर प्रवाह पर निर्भर करता है।
पारिस्थितिक तंत्र में, उनके सदस्यों की स्थिति और महत्वपूर्ण गतिविधि और आबादी के अनुपात में परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। किसी भी समुदाय में होने वाले विविध परिवर्तन दो मुख्य प्रकारों में आते हैं: चक्रीय और प्रगतिशील।
एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एक जीवमंडल है जो पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता और स्थिरता की विशेषता है।
1. पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा और संरचना
1 पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा
जीवित जीव और उनका निर्जीव (अजैविक) पर्यावरण एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं और निरंतर संपर्क में हैं। किसी पारितंत्र की कोई भी इकाई (जैवतंत्र) एक पारिस्थितिक तंत्र है। एक पारिस्थितिक तंत्र, या पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी में बुनियादी कार्यात्मक इकाई है, क्योंकि इसमें जीव और निर्जीव पर्यावरण शामिल हैं - ऐसे घटक जो पृथ्वी पर मौजूद जीवन को बनाए रखने के लिए एक-दूसरे के गुणों और आवश्यक परिस्थितियों को परस्पर प्रभावित करते हैं। "पारिस्थितिकी तंत्र" शब्द पहली बार 1935 में अंग्रेजी पारिस्थितिकीविज्ञानी ए. टैन्सले द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में, पारिस्थितिकी तंत्र की निम्नलिखित परिभाषा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र जीवों और अकार्बनिक घटकों का कोई संग्रह है जिसमें पदार्थों का संचलन हो सकता है। एन.एफ. के अनुसार रीमर्स (1990), एक पारिस्थितिकी तंत्र जीवित प्राणियों और उसके आवास का कोई भी समुदाय है, जो एक एकल कार्यात्मक संपूर्ण में एकजुट होता है, जो व्यक्तिगत पर्यावरणीय घटकों के बीच मौजूद अन्योन्याश्रय और कारण-और-प्रभाव संबंधों के आधार पर उत्पन्न होता है। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि जीवित जीवों के समुदाय (बायोसेनोसिस) के साथ एक विशिष्ट भौतिक-रासायनिक वातावरण (बायोटोप) का संयोजन एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। ए. टैन्सले (1935) ने निम्नलिखित संबंध प्रस्तावित किया:
पारिस्थितिकी तंत्र = बायोटोप + बायोसेनोसिस
वी.एन. की परिभाषा के अनुसार. सुकाचेव के अनुसार, बायोजियोसेनोसिस "पृथ्वी की सतह की एक निश्चित सीमा पर सजातीय प्राकृतिक घटनाओं (वायुमंडल, चट्टान, मिट्टी और जल विज्ञान संबंधी स्थितियों) का एक समूह है, जिसमें इन घटकों की बातचीत की अपनी विशेष विशिष्टता होती है जो इसे बनाते हैं और एक निश्चित प्रकार के होते हैं आपस में और अन्य प्राकृतिक घटनाओं के बीच पदार्थ और ऊर्जा का आदान-प्रदान और निरंतर गति और विकास में आंतरिक रूप से विरोधाभासी द्वंद्वात्मक एकता का प्रतिनिधित्व करना।"
पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणाओं के अलावा ए. टेन्सले और बायोजियोसेनोसिस वी.एन. सुकाचेव ने एफ. इवांस (1956) का नियम तैयार किया, जिन्होंने पर्यावरण के साथ बातचीत करने वाले किसी भी सुपरऑर्गेनिज्मल जीवित सिस्टम को नामित करने के लिए "पारिस्थितिकी तंत्र" शब्द का बिल्कुल "आयामहीन" उपयोग करने का प्रस्ताव रखा। हालाँकि, कई लेखकों ने "पारिस्थितिकी तंत्र" शब्द को बायोजियोसेनोसिस का अर्थ दिया है, अर्थात। प्राथमिक पारिस्थितिकी तंत्र, और साथ ही जीवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र तक सुप्रा-बायोजियोकेनोटिक संरचनाओं के पदानुक्रम में उच्चतर।
2 पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण
पृथ्वी पर मौजूद पारिस्थितिक तंत्र विविध हैं। इसमें माइक्रोइकोसिस्टम (उदाहरण के लिए, एक सड़ते हुए पेड़ का तना), मेसोइकोसिस्टम (जंगल, तालाब, आदि), मैक्रोइकोसिस्टम (महाद्वीप, महासागर, आदि) और वैश्विक जीवमंडल हैं।
बड़े स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बायोम कहा जाता है। प्रत्येक बायोम में कई छोटे, परस्पर जुड़े हुए पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के कई वर्गीकरण हैं:
सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन
रेगिस्तान: घास और झाड़ियाँ चापराल - बरसाती सर्दियाँ और शुष्क ग्रीष्मकाल वाले क्षेत्र
उष्णकटिबंधीय ग्रासलेनज़ और सवाना
समशीतोष्ण मैदान
शांत पर्णपाती जंगल
बोरियल शंकुधारी वन
टुंड्रा: आर्कटिक और अल्पाइन
मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार:
रिबन (शांत पानी): झीलें, तालाब, आदि।
लोटिक (बहता पानी): नदियाँ, झरने आदि।
आर्द्रभूमियाँ: दलदल और दलदली वन
समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार
खुला महासागर (पेलजिक)
महाद्वीपीय शेल्फ जल (तटीय जल)
उत्थान क्षेत्र (उत्पादक मत्स्य पालन वाले उपजाऊ क्षेत्र)
ज्वारनदमुख (तटीय खाड़ियाँ, जलडमरूमध्य, नदी के मुहाने, नमक दलदल, आदि)। यहां स्थलीय बायोम प्राकृतिक या मूल वनस्पति विशेषताओं द्वारा प्रतिष्ठित हैं, और जलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार भूवैज्ञानिक और भौतिक विशेषताओं द्वारा प्रतिष्ठित हैं। सूचीबद्ध मुख्य प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र उस पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें मानव सभ्यता विकसित हुई और पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने वाले मुख्य जैविक समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
3 मैक्रोइकोसिस्टम की ज़ोनिंग
पारिस्थितिक तंत्र के भौगोलिक वितरण का अध्ययन केवल बड़ी पारिस्थितिक इकाइयों - मैक्रोइकोसिस्टम के स्तर पर ही किया जा सकता है, जिन्हें महाद्वीपीय पैमाने पर माना जाता है। पारिस्थितिक तंत्र अव्यवस्था में बिखरे हुए नहीं हैं; इसके विपरीत, वे क्षैतिज (अक्षांश में) और लंबवत (ऊंचाई में) दोनों, काफी नियमित क्षेत्रों में समूहीकृत हैं। इसकी पुष्टि ए.ए. के भौगोलिक क्षेत्रीकरण के आवधिक नियम से होती है। ग्रिगोरिएवा - एम.आई. बुड्यको: पृथ्वी के भौतिक-भौगोलिक क्षेत्रों में परिवर्तन के साथ, समान परिदृश्य क्षेत्र और उनके कुछ सामान्य गुण समय-समय पर दोहराए जाते हैं। जीवन के ज़मीनी-वायु पर्यावरण पर विचार करते समय इस पर भी चर्चा की गई। कानून द्वारा स्थापित आवधिकता इस तथ्य में प्रकट होती है कि शुष्कता सूचकांक का मान विभिन्न क्षेत्रों में 0 से 4-5 तक भिन्न होता है, ध्रुवों और भूमध्य रेखा के बीच तीन बार वे एकता के करीब होते हैं। ये मूल्य परिदृश्यों की उच्चतम जैविक उत्पादकता के अनुरूप हैं।
एक पदानुक्रमित स्तर की प्रणालियों की एक श्रृंखला में गुणों की आवधिक पुनरावृत्ति संभवतः ब्रह्मांड का एक सामान्य कानून है, जिसे प्रणालीगत समुच्चय की संरचना में आवधिकता के कानून के रूप में तैयार किया गया है, या सिस्टम-आवधिक कानून - एक स्तर की विशिष्ट प्राकृतिक प्रणाली ( संगठन के उपस्तर) ऊपरी और निचले सिस्टम स्पेस-टाइम सीमाओं के भीतर रूपात्मक रूप से समान संरचनाओं की एक आवधिक या दोहराई जाने वाली श्रृंखला का गठन करते हैं, जिसके परे किसी दिए गए स्तर पर सिस्टम का अस्तित्व असंभव हो जाता है। वे एक अस्थिर स्थिति में चले जाते हैं या संगठन के दूसरे स्तर सहित किसी अन्य सिस्टम संरचना में बदल जाते हैं।
तापमान और वर्षा पृथ्वी की सतह पर मुख्य स्थलीय बायोम का स्थान निर्धारित करते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में काफी लंबे समय तक तापमान और वर्षा के पैटर्न को हम जलवायु कहते हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु भिन्न-भिन्न है। वार्षिक वर्षा 0 से 2500 मिमी या अधिक तक होती है। तापमान और वर्षा की व्यवस्थाएं बहुत अलग-अलग तरीकों से मिलती हैं।
जलवायु परिस्थितियों की विशिष्टताएँ, बदले में, किसी विशेष बायोम के विकास को निर्धारित करती हैं।
भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक, विभिन्न गोलार्धों के बायोम के वितरण में एक निश्चित समरूपता दिखाई देती है:
उष्णकटिबंधीय वर्षावन (उत्तरी दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, भूमध्यरेखीय अफ्रीका के पश्चिमी और मध्य भाग, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र, भारतीय और प्रशांत महासागरों के द्वीप)। जलवायु ऋतु परिवर्तन (भूमध्य रेखा से निकटता) के बिना है, औसत वार्षिक तापमान 17 डिग्री सेल्सियस (आमतौर पर 28 डिग्री सेल्सियस) से ऊपर है, औसत वार्षिक वर्षा 2400 मिमी से अधिक है।
वनस्पति: वनों का प्रभुत्व है। कुछ प्रकार के पेड़ 60 मीटर तक ऊंचे होते हैं। उनके तनों और शाखाओं पर एपिफाइटिक पौधे होते हैं, जिनकी जड़ें मिट्टी तक नहीं पहुंचती हैं, और लकड़ी की लताएं होती हैं जो मिट्टी में जड़ें जमा लेती हैं और पेड़ों के शीर्ष पर चढ़ जाती हैं। यह सब एक मोटी छतरी का निर्माण करते हैं।
जीव-जंतु: संयुक्त रूप से अन्य सभी बायोम की तुलना में प्रजातियों की संरचना अधिक समृद्ध है। विशेष रूप से असंख्य उभयचर, सरीसृप और पक्षी (मेंढक, छिपकली, सांप, तोते), बंदर और अन्य छोटे स्तनधारी, चमकीले रंगों वाले विदेशी कीड़े और जलाशयों में चमकीले रंग की मछलियाँ हैं।
विशेषताएं: मिट्टी अक्सर पतली और खराब होती है, अधिकांश पोषक तत्व जड़ वाली वनस्पति की सतह बायोमास में निहित होते हैं।
2. सवाना (उपभूमध्यरेखीय अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा)। वर्ष के अधिकांश समय जलवायु शुष्क और गर्म रहती है। गीले मौसम के दौरान भारी वर्षा। तापमान: औसत वार्षिक-उच्च। वर्षा 750-1650 मिमी/वर्ष होती है, मुख्यतः वर्षा ऋतु के दौरान। वनस्पति - दुर्लभ पर्णपाती पेड़ों के साथ ब्लूग्रास (अनाज) पौधे। जीव-जंतु: बड़े शाकाहारी स्तनधारी, जैसे मृग, ज़ेबरा, जिराफ़, गैंडा, शिकारी - शेर, तेंदुए, चीता।
रेगिस्तान (अफ्रीका के कुछ क्षेत्र, उदाहरण के लिए सहारा; मध्य पूर्व और मध्य एशिया, ग्रेट बेसिन और दक्षिण-पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको, आदि)। जलवायु बहुत शुष्क है. तापमान - गर्म दिन और ठंडी रातें। वर्षा 250 मिमी/वर्ष से कम है। वनस्पति: विरल झाड़ियाँ, अक्सर कांटेदार, कभी-कभी कैक्टि और कम घास, दुर्लभ बारिश के बाद जल्दी से जमीन को फूलों के कालीन से ढक देती हैं। पौधों में व्यापक सतह जड़ प्रणाली होती है जो दुर्लभ वर्षा से नमी को रोकती है, साथ ही नल की जड़ें भी होती हैं जो जमीन में भूजल स्तर (30 मीटर और अधिक गहराई) तक प्रवेश करती हैं। जीव-जंतु: विभिन्न कृंतक (कंगारू चूहा, आदि), टोड, छिपकली, सांप और अन्य सरीसृप, उल्लू, चील, गिद्ध, छोटे पक्षी और बड़ी मात्रा में कीड़े।
4. स्टेप्स (उत्तरी अमेरिका का केंद्र, रूस, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण-पूर्व)। जलवायु मौसमी है. तापमान - गर्मियों का तापमान मध्यम गर्म से गर्म तक होता है, सर्दियों का तापमान 0°C से नीचे होता है। वर्षा - 750-2000 मिमी/वर्ष। वनस्पति: उत्तरी अमेरिका के कुछ मैदानी इलाकों में 2 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई तक या 50 सेमी तक ब्लूग्रास (अनाज) का प्रभुत्व है, उदाहरण के लिए, रूसी स्टेप्स में, गीले क्षेत्रों में अलग-अलग पेड़ और झाड़ियाँ हैं। जीव: बड़े शाकाहारी स्तनधारी - बाइसन, प्रोंगहॉर्न मृग (उत्तरी अमेरिका), जंगली घोड़े (यूरेशिया), कंगारू (ऑस्ट्रेलिया), जिराफ, ज़ेबरा, सफेद गैंडा, मृग (अफ्रीका); शिकारियों में कोयोट, शेर, तेंदुए, चीता, लकड़बग्घा, विभिन्न प्रकार के पक्षी और छोटे बिल में रहने वाले स्तनधारी जैसे खरगोश, ज़मीनी गिलहरी और एर्डवार्क शामिल हैं।
5. शीतोष्ण वन (पश्चिमी यूरोप, पूर्वी एशिया, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका)। जलवायु - मौसमी, सर्दियों का तापमान 0 से नीचे 0C. वर्षा - 750-2000 मिमी/वर्ष। वनस्पति: 35-45 मीटर ऊंचे (ओक, हिकॉरी, मेपल), झाड़ीदार झाड़ियाँ, काई, लाइकेन तक चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती पेड़ों के जंगलों का प्रभुत्व है। जीव-जंतु: स्तनधारी (सफेद पूंछ वाले हिरण, साही, रैकून, ओपस्सम, गिलहरी, खरगोश, छछूंदर), पक्षी (वॉर्बलर, कठफोड़वा, ब्लैकबर्ड, उल्लू, बाज़), सांप, मेंढक, सैलामैंडर, मछली (ट्राउट, पर्च, कैटफ़िश, आदि) .), प्रचुर मृदा सूक्ष्म जीव (चित्र 12.3)। बायोटा मौसमी जलवायु के अनुकूल है: सर्दियों के महीनों में हाइबरनेशन, प्रवासन, सुस्ती। 6. शंकुधारी वन, टैगा (उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तरी क्षेत्र)। जलवायु लंबी और ठंडी सर्दियाँ होती है, जिसमें कुछ वर्षा बर्फ के रूप में गिरती है। वनस्पति: सदाबहार शंकुधारी वनों का प्रभुत्व है, जिनमें अधिकतर स्प्रूस, देवदार और देवदार हैं। जीव-जंतु: बड़े शाकाहारी अनगुलेट्स (खच्चर हिरण, बारहसिंगा), छोटे शाकाहारी स्तनधारी (खरगोश, गिलहरी, कृंतक), भेड़िया, लिनेक्स, लोमड़ी, काला भालू, भूरा भालू, वूल्वरिन, मिंक और अन्य शिकारी, छोटी गर्मियों में कई खून चूसने वाले कीड़े समय। ध्रुवीय दिन और ध्रुवीय रातों के साथ जलवायु बहुत ठंडी है। औसत वार्षिक तापमान - 5°C से नीचे है। छोटी गर्मी के कुछ हफ्तों में, ज़मीन एक मीटर से अधिक गहराई तक नहीं पिघलती। वर्षा 250 मिमी/वर्ष से कम है। वनस्पति: धीरे-धीरे बढ़ने वाले लाइकेन, काई, घास और सेज और बौनी झाड़ियों का प्रभुत्व है। जीव-जंतु: बड़े शाकाहारी अनगुलेट्स (हिरन, कस्तूरी बैल), छोटे बिल में रहने वाले स्तनधारी (पूरे वर्ष, उदाहरण के लिए, लेमिंग्स), शिकारी जो सर्दियों में छलावरण सफेद रंग प्राप्त कर लेते हैं (आर्कटिक लोमड़ी, लिनेक्स, इर्मिन, बर्फीला उल्लू)। छोटी गर्मियों में, टुंड्रा में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी घोंसला बनाते हैं, उनमें से विशेष रूप से कई जलपक्षी होते हैं, जो यहां प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कीड़ों और मीठे पानी के अकशेरुकी जीवों को खाते हैं। भूमि पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्षेत्र, विशेष रूप से स्पष्ट राहत वाले स्थानों में, भी बहुत स्पष्ट है। आर्द्रता मुख्य कारक है जो बायोम के प्रकार को निर्धारित करती है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने से वन वनस्पति का विकास होता है। तापमान जंगल के प्रकार को निर्धारित करता है। स्टेपी और रेगिस्तानी बायोम में स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। ठंडे क्षेत्रों में वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन कम वार्षिक वर्षा मात्रा के साथ होता है, क्योंकि कम तापमान पर वाष्पीकरण के कारण कम पानी बर्बाद होता है। तापमान केवल पर्माफ्रॉस्ट के साथ अत्यधिक ठंडी स्थितियों में ही एक प्रमुख कारक बन जाता है। इस प्रकार, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना काफी हद तक उनके कार्यात्मक "उद्देश्य" पर निर्भर करती है और इसके विपरीत। एन.एफ. के अनुसार रीमर्स (1994), यह पारिस्थितिक संपूरकता (पूरकता) के सिद्धांत में परिलक्षित होता है: पारिस्थितिकी तंत्र का कोई भी कार्यात्मक हिस्सा (पारिस्थितिक घटक, तत्व, आदि) अन्य कार्यात्मक पूरक भागों के बिना मौजूद नहीं हो सकता है। इसके करीब और इसका विस्तार करना पारिस्थितिक अनुरूपता (पत्राचार) का सिद्धांत है:। कार्यात्मक रूप से एक-दूसरे के पूरक होते हुए, पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित घटक इसके लिए उपयुक्त अनुकूलन विकसित करते हैं, जो कि अजैविक पर्यावरण की स्थितियों के साथ समन्वित होता है, जो बड़े पैमाने पर समान जीवों (जैव जलवायु, आदि) द्वारा रूपांतरित होता है, अर्थात। पत्राचार की एक दोहरी श्रृंखला है - जीवों और उनके आवास के बीच - बाहरी और सेनोसिस द्वारा निर्मित। 4 पारिस्थितिकी तंत्र संरचना पोषी संरचना (ग्रीक ट्रॉफ - पोषण से) के दृष्टिकोण से, पारिस्थितिकी तंत्र को दो स्तरों में विभाजित किया जा सकता है: ऊपरी - ऑटोट्रॉफ़िक (स्व-भक्षण) स्तर, या "हरित बेल्ट", जिसमें पौधे या क्लोरोफिल युक्त उनके हिस्से शामिल हैं, जहां गिनती ऊर्जा का निर्धारण और सरल अकार्बनिक यौगिकों का उपयोग प्रबल होता है। निचली परत हेटरोट्रॉफ़िक (दूसरों द्वारा पोषित) परत या मिट्टी और तलछट, सड़ने वाले पदार्थ, जड़ों आदि की "भूरी बेल्ट" है, जिसमें जटिल यौगिकों का उपयोग, परिवर्तन और अपघटन प्रमुख होता है। जैविक दृष्टिकोण से, निम्नलिखित घटकों को एक पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है: एक पारिस्थितिकी तंत्र में, श्रेणियों के बीच भोजन और ऊर्जा संबंध हमेशा स्पष्ट होते हैं और निम्न दिशा में चलते हैं: स्वपोषी - विषमपोषी या अधिक पूर्ण रूप में; स्वपोषी -> उपभोक्ता -> अपघटक (विनाशक)। पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। सूर्य द्वारा पृथ्वी ग्रह पर भेजा गया ऊर्जा प्रवाह (टी.ए. अकीमोवा, वी.वी. खास्किन, 1994 के अनुसार) प्रति वर्ष 20 मिलियन ईजे से अधिक है। इस प्रवाह का केवल एक चौथाई भाग ही वायुमंडल की सीमा तक पहुँचता है। इसमें से लगभग 70% वायुमंडल द्वारा परावर्तित, अवशोषित और लंबी-तरंग अवरक्त विकिरण के रूप में उत्सर्जित होता है। पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाला सौर विकिरण 1.54 मिलियन EJ प्रति वर्ष है। ऊर्जा की यह विशाल मात्रा 20वीं शताब्दी के अंत में मानवता की संपूर्ण ऊर्जा का 5000 गुना है और कम से कम 100 मिलियन वर्षों में संचित जैविक मूल के सभी उपलब्ध जीवाश्म ईंधन संसाधनों की ऊर्जा का 5.5 गुना है। ग्रह की सतह तक पहुंचने वाली अधिकांश सौर ऊर्जा सीधे गर्मी, पानी या मिट्टी को गर्म करने में परिवर्तित हो जाती है, जो बदले में हवा को गर्म करती है। यह ऊष्मा जल चक्र, वायु धाराओं और समुद्री धाराओं के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है जो मौसम निर्धारित करती है, और धीरे-धीरे बाहरी अंतरिक्ष में छोड़ी जाती है, जहां यह खो जाती है। ऊर्जा के इस प्राकृतिक प्रवाह में पारिस्थितिक तंत्र का स्थान निर्धारित करने के लिए, यह जानना महत्वपूर्ण है कि चाहे वे कितने भी व्यापक और जटिल क्यों न हों, वे इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग करते हैं। इसका तात्पर्य पारिस्थितिक तंत्र के कामकाज के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है: वे गैर-प्रदूषणकारी और लगभग शाश्वत सौर ऊर्जा के कारण मौजूद हैं, जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत स्थिर और प्रचुर है। आइए हम सौर ऊर्जा की प्रत्येक सूचीबद्ध विशेषता के बारे में अधिक विस्तार से बताएं: 2. पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाले कारक 1 पदार्थ चक्र दोनों चक्र परस्पर जुड़े हुए हैं और मानो एक ही प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि वायुमंडल में मौजूद सभी ऑक्सीजन 2000 वर्षों में जीवों के माध्यम से चक्रित होती है (श्वसन के दौरान संयुक्त और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जारी होती है), वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 300 वर्षों में विपरीत दिशा में चक्र करती है, और पृथ्वी पर सारा पानी है 2,000,000 वर्षों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के माध्यम से विघटित और पुनः निर्मित। पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक कारकों और जीवित जीवों की परस्पर क्रिया के साथ वैकल्पिक कार्बनिक और खनिज यौगिकों के रूप में बायोटोप और बायोकेनोसिस के बीच पदार्थ का निरंतर संचलन होता है। जीवित जीवों और अकार्बनिक पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों का आदान-प्रदान, जिसके विभिन्न चरण एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर होते हैं, को जैव-भू-रासायनिक परिसंचरण, या जैव-भू-रासायनिक चक्र कहा जाता है। जल चक्र। स्थानांतरित द्रव्यमान और ऊर्जा खपत के संदर्भ में पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण चक्र ग्रहीय जल विज्ञान चक्र - जल चक्र है। इसमें हर सेकंड 16.5 मिलियन घन मीटर पानी शामिल होता है और इस पर 40 बिलियन मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा खर्च होती है, (टी.ए. अकीमोवा वी.वी. हास्किन के अनुसार, (1994))। लेकिन यह चक्र केवल जलराशि का स्थानांतरण नहीं है। ये चरण परिवर्तन, समाधान और निलंबन का निर्माण, अवक्षेपण, क्रिस्टलीकरण, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाएं, साथ ही विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं। इसी वातावरण में जीवन उत्पन्न हुआ और जारी है। जल जीवन के लिए आवश्यक मूल तत्व है। मात्रात्मक रूप से, यह जीवित पदार्थ का सबसे आम अकार्बनिक घटक है। मनुष्यों में, शरीर के वजन का 63% पानी होता है, मशरूम में - 80%, पौधों में - 80-90%, और कुछ जेलिफ़िश में - 98% पानी, जैसा कि हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, जैविक चक्र में भाग लेता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो इसकी कुल मात्रा का केवल एक छोटा सा हिस्सा बनाता है। तरल, ठोस और वाष्प अवस्था में, पानी जीवमंडल के सभी तीन मुख्य घटकों में मौजूद है: वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। सभी जल "जलमंडल" की सामान्य अवधारणा से एकजुट हैं। जलमंडल के घटक निरंतर आदान-प्रदान और अंतःक्रिया द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। जल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में निरंतर गति करते हुए छोटे-बड़े चक्र बनाता रहता है। समुद्र की सतह से पानी का वाष्पीकरण, वायुमंडल में जलवाष्प का संघनन और समुद्र की सतह पर वर्षा एक छोटे चक्र का निर्माण करती है। जब जलवाष्प को वायु धाराओं द्वारा भूमि पर ले जाया जाता है, तो चक्र बहुत अधिक जटिल हो जाता है। इस मामले में, वर्षा का एक हिस्सा वाष्पित हो जाता है और वायुमंडल में वापस चला जाता है, दूसरा नदियों और जलाशयों को पोषण देता है, लेकिन अंततः नदी और भूमिगत अपवाह के माध्यम से समुद्र में लौट आता है, जिससे बड़ा चक्र पूरा होता है। बायोटिक (जैविक) चक्र. जैविक (जैविक) चक्र मिट्टी, पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों के बीच पदार्थों के परिसंचरण को संदर्भित करता है। जैविक (जैविक) चक्र मिट्टी, पानी और वातावरण से जीवित जीवों में रासायनिक तत्वों का प्रवाह, आने वाले तत्वों का नए जटिल यौगिकों में परिवर्तन और कार्बनिक के हिस्से की वार्षिक गिरावट के साथ जीवन की प्रक्रिया में वापस लौटना है। पारिस्थितिकी तंत्र संरचना में शामिल पदार्थ या पूरी तरह से मृत जीवों के साथ। अब हम जैविक चक्र को चक्रीय रूप में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय जैविक चक्र (टी.ए. अकीमोवा, वी.वी., खस्किन के अनुसार) में आदिम एककोशिकीय उत्पादक (पी) और डीकंपोजर-विनाशक (डी) शामिल थे। सूक्ष्मजीव तेजी से गुणा करने और विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करने में सक्षम हैं, उदाहरण के लिए, अपने आहार में सभी प्रकार के सब्सट्रेट्स - कार्बन स्रोतों - का उपयोग करते हैं। उच्चतर जीवों में ऐसी क्षमताएँ नहीं होतीं। संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र में ये सूक्ष्मजीवों की नींव पर एक संरचना के रूप में मौजूद हो सकते हैं। सबसे पहले, बहुकोशिकीय पौधे (पी) विकसित होते हैं - उच्च उत्पादक। एककोशिकीय जीवों के साथ मिलकर, वे सौर विकिरण की ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। इसके बाद, प्राथमिक उपभोक्ता जुड़े हुए हैं - शाकाहारी जानवर (टी), और फिर मांसाहारी उपभोक्ता। हमने भूमि के जैविक चक्र की जांच की। यह पूरी तरह से जलीय पारिस्थितिक तंत्र के जैविक चक्र पर लागू होता है, उदाहरण के लिए, महासागर। सभी जीव जैविक चक्र में एक निश्चित स्थान पर कब्जा कर लेते हैं और प्राप्त ऊर्जा प्रवाह की शाखाओं को बदलने और बायोमास को स्थानांतरित करने का अपना कार्य करते हैं। एकल-कोशिका विघटित करने वालों (विनाशकों) की एक प्रणाली सभी को एकजुट करती है, उनके पदार्थों का प्रतिरूपण करती है और सामान्य चक्र को बंद कर देती है। वे नई और नई क्रांतियों के लिए आवश्यक सभी तत्वों को जीवमंडल के अजैविक वातावरण में लौटा देते हैं। जैविक चक्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण एक शक्तिशाली प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके चक्र में प्रतिवर्ष जीवमंडल के पदार्थ का विशाल द्रव्यमान शामिल होता है और इसकी उच्च ऑक्सीजन क्षमता निर्धारित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के कारण कार्बनिक पदार्थ संश्लेषित होते हैं और मुक्त ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण के प्रत्यक्ष उत्पाद विभिन्न कार्बनिक यौगिक हैं, और सामान्य तौर पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। ऑक्सीजन की भागीदारी के साथ प्रकाश संश्लेषण, तथाकथित ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के अलावा, हमें ऑक्सीजन मुक्त प्रकाश संश्लेषण, या केमोसिंथेसिस पर भी ध्यान देना चाहिए। रसायन संश्लेषक जीवों में नाइट्रिफायर, कार्बोक्सीडोबैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, थियोनिक आयरन बैक्टीरिया और हाइड्रोजन बैक्टीरिया शामिल हैं। इनका नाम उनके ऑक्सीकरण सब्सट्रेट्स के नाम पर रखा गया है, जो NH3, NO2, CO, H2S, S, Fe2+, H2 हो सकते हैं। कुछ प्रजातियाँ बाध्यकारी केमोलिथोऑटोट्रॉफ़ हैं, अन्य ऐच्छिक हैं। उत्तरार्द्ध में कार्बोक्सीडोबैक्टीरिया और हाइड्रोजन बैक्टीरिया शामिल हैं। केमोसिंथेसिस गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट की विशेषता है। प्रकाश संश्लेषण, कुछ अपवादों के साथ, पृथ्वी की पूरी सतह पर होता है, एक विशाल भू-रासायनिक प्रभाव पैदा करता है और इसे पूरे जीवमंडल के कार्बनिक - जीवित पदार्थ के निर्माण में सालाना शामिल कार्बन के पूरे द्रव्यमान की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बनिक पदार्थ के निर्माण से जुड़े पदार्थ के सामान्य चक्र में एन, पी, एस जैसे रासायनिक तत्वों के साथ-साथ धातुएं - के, सीए, एमजी, ना, अल भी शामिल होते हैं। जब कोई जीव मर जाता है, तो विपरीत प्रक्रिया होती है - ऑक्सीकरण, क्षय आदि के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। अंतिम अपघटन उत्पादों के निर्माण के साथ। पृथ्वी के जीवमंडल में, यह प्रक्रिया इस तथ्य की ओर ले जाती है कि जीवित पदार्थ के बायोमास की मात्रा कुछ हद तक स्थिर रहती है। पारिस्थितिकमंडल का बायोमास (2 10|2t) पृथ्वी की पपड़ी के द्रव्यमान (2 .10|9t) से सात कोटि कम परिमाण है। पृथ्वी के पौधे प्रतिवर्ष 1.6.10"% या पारिस्थितिकमंडल के बायोमास के 8% के बराबर कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन करते हैं। विध्वंसक, जो ग्रह के जीवों के कुल बायोमास का 1% से भी कम बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थ के एक द्रव्यमान को संसाधित करते हैं जो कि 10 है अपने स्वयं के बायोमास से कई गुना अधिक। औसतन, बायोमास नवीकरण की अवधि 12.5 वर्ष है। आइए मान लें कि जीवित पदार्थ का द्रव्यमान और जीवमंडल की उत्पादकता कैंब्रियन से वर्तमान (530 मिलियन वर्ष) तक समान थी, तब वैश्विक जैविक चक्र से गुजरने वाले और ग्रह पर जीवन द्वारा उपयोग किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा 2.10" 2-5,ZL08/12.5=8.5L0|9t होगी, जो पृथ्वी की पपड़ी के द्रव्यमान का 4 गुना है। इन गणनाओं के संबंध में एन.एस. पेचुर्किन (1988) ने लिखा: "हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर को बनाने वाले परमाणु प्राचीन बैक्टीरिया, डायनासोर और मैमथ में थे।" परमाणुओं के बायोजेनिक प्रवास का नियम वी.आई. वर्नाडस्की कहते हैं: "पृथ्वी की सतह पर और संपूर्ण जीवमंडल में रासायनिक तत्वों का प्रवासन या तो जीवित पदार्थ (बायोजेनिक प्रवासन) की प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ होता है, या यह ऐसे वातावरण में होता है जिसकी भू-रासायनिक विशेषताएं (O2, CO2, H2, आदि) निर्धारित जीवित पदार्थ हैं, दोनों वह जो वर्तमान में जीवमंडल में निवास करता है और जिसने पूरे भूवैज्ञानिक इतिहास में पृथ्वी पर कार्य किया है।" में और। 1928-1930 में वर्नाडस्की जीवमंडल में प्रक्रियाओं के संबंध में अपने गहन सामान्यीकरण में, उन्होंने जीवित पदार्थ के पांच मुख्य जैव-रासायनिक कार्यों का एक विचार दिया। पहला कार्य गैस है. दूसरा कार्य है एकाग्रता. तीसरा कार्य रेडॉक्स है। चौथा कार्य जैवरासायनिक है। पांचवां कार्य मानव जाति की जैव-भू-रासायनिक गतिविधि है, जो उद्योग, परिवहन और कृषि की जरूरतों के लिए पृथ्वी की पपड़ी में पदार्थ की बढ़ती मात्रा को कवर करती है। जैविक चक्र विभिन्न प्राकृतिक क्षेत्रों में भिन्न होता है और इसे संकेतकों के एक सेट के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है: पौधे का बायोमास, कूड़ा, कूड़ा, बायोमास में निर्धारित तत्वों की मात्रा, आदि। कुल बायोमास वन क्षेत्र में सबसे अधिक है, और वनों में भूमिगत अंगों का अनुपात सबसे कम है। इसकी पुष्टि जैविक चक्र तीव्रता सूचकांक द्वारा की जाती है - कूड़े के द्रव्यमान का कूड़े के उस हिस्से से अनुपात जो इसे बनाता है। कार्बन चक्र। सभी जैव-भू-रासायनिक चक्रों में से, कार्बन चक्र निस्संदेह सबसे तीव्र है। कार्बन विभिन्न अकार्बनिक माध्यमों के बीच और जीवित जीवों के समुदायों के भीतर खाद्य जाल के माध्यम से उच्च दर पर प्रसारित होता है। CO और CO2 कार्बन चक्र में एक निश्चित भूमिका निभाते हैं। अक्सर पृथ्वी के जीवमंडल में, कार्बन को CO2 के सबसे गतिशील रूप में दर्शाया जाता है। जीवमंडल में प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत ज्वालामुखीय गतिविधि है जो पृथ्वी की पपड़ी के मेंटल और निचले क्षितिज के धर्मनिरपेक्ष क्षरण से जुड़ी है। जीवमंडल में CO2 का प्रवासन दो प्रकार से होता है। पहला तरीका प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज और अन्य कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के साथ इसे अवशोषित करना है जिससे सभी पौधों के ऊतकों का निर्माण होता है। वे बाद में खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य सभी जीवित प्राणियों के ऊतकों का निर्माण करते हैं। सतह पर पौधों और जानवरों की मृत्यु के साथ, CO2 के निर्माण के साथ कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। जब कार्बनिक पदार्थ जलाए जाते हैं तो कार्बन परमाणु भी वायुमंडल में लौट आते हैं। कार्बन चक्र की एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प विशेषता यह है कि सुदूर भूवैज्ञानिक युगों में, सैकड़ों लाखों साल पहले, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं में निर्मित कार्बनिक पदार्थ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उपभोक्ताओं या डीकंपोजर द्वारा उपयोग नहीं किया जाता था, बल्कि स्थलमंडल में जमा होता था। जीवाश्म ईंधन के रूप में: तेल, कोयला, तेल शेल, पीट, आदि। हमारे औद्योगिक समाज की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इन जीवाश्म ईंधन का भारी मात्रा में खनन किया जाता है। इसे जलाकर हम एक तरह से कार्बन चक्र पूरा करते हैं। दूसरे तरीके में, विभिन्न जलाशयों में कार्बोनेट प्रणाली बनाकर कार्बन प्रवासन किया जाता है, जहां CO2 H2CO3, HCO, CO3 में परिवर्तित हो जाता है। पानी में घुले कैल्शियम (या मैग्नीशियम) की मदद से, बायोजेनिक और एबोजेनिक मार्गों के माध्यम से कार्बोनेट (CaCO3) अवक्षेपित होते हैं। चूना पत्थर की मोटी परतें बन जाती हैं। ए.बी. के अनुसार रोनोव के अनुसार, प्रकाश संश्लेषक उत्पादों में दबे हुए कार्बन का कार्बोनेट चट्टानों में कार्बन से अनुपात 1:4 है। बड़े कार्बन चक्र के साथ-साथ भूमि की सतह और समुद्र में कई छोटे कार्बन चक्र भी होते हैं। सामान्य तौर पर, मानवजनित हस्तक्षेप के बिना, जैव-भू-रासायनिक जलाशयों में कार्बन सामग्री: जीवमंडल (बायोमास + मिट्टी और मलबे), तलछटी चट्टानें, वायुमंडल और जलमंडल, उच्च स्तर की स्थिरता के साथ बनाए रखा जाता है (टी.ए. अकीमोवा, वी.वी. हास्किन (1994 के अनुसार) ). कार्बन का निरंतर आदान-प्रदान, एक ओर, जीवमंडल के बीच, और दूसरी ओर, वायुमंडल और जलमंडल के बीच, जीवित पदार्थ के गैस कार्य द्वारा निर्धारित होता है - प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और विनाश की प्रक्रियाएं, और लगभग 6-1010 टन/वर्ष। वायुमंडल और जलमंडल में कार्बन का प्रवाह होता है और ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान औसतन 4.5 106 टन/वर्ष. जीवाश्म ईंधन (तेल, गैस, कोयला, आदि) में कार्बन का कुल द्रव्यमान 3.2*1015 टन अनुमानित है, जो 7 मिलियन टन/वर्ष की औसत संचय दर से मेल खाता है। यह मात्रा परिसंचारी कार्बन के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य है और, जैसे कि, चक्र से बाहर हो गई और इसमें खो गई। इसलिए, चक्र के खुलेपन (अपूर्णता) की डिग्री 10"4, या 0.01% है, और, तदनुसार, बंद होने की डिग्री 99.99 है। इसका मतलब है, एक तरफ, प्रत्येक कार्बन परमाणु ने चक्र में भाग लिया चक्र से बाहर गिरने से पहले हजारों बार, गहराई में समाप्त हो गए। दूसरी ओर, जीवमंडल में कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण और क्षय के प्रवाह को बहुत उच्च परिशुद्धता के साथ एक दूसरे से समायोजित किया जाता है। मोबाइल कार्बन स्टॉक का 0.2% निरंतर प्रचलन में है। बायोमास कार्बन का नवीनीकरण 12 वर्षों में, वायुमंडल में - 8 वर्षों में होता है। ऑक्सीजन चक्र. ऑक्सीजन (O2) हमारे ग्रह पर अधिकांश जीवित जीवों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मात्रात्मक दृष्टि से यह सजीव पदार्थ का मुख्य घटक है। उदाहरण के लिए, यदि हम ऊतकों में मौजूद पानी को ध्यान में रखें, तो मानव शरीर में 62.8% ऑक्सीजन और 19.4% कार्बन होता है। सामान्यतः जीवमंडल में कार्बन एवं हाइड्रोजन की तुलना में यह तत्व सरल पदार्थों में प्रमुख है। जीवमंडल के भीतर, जीवित जीवों या मृत्यु के बाद उनके अवशेषों के साथ ऑक्सीजन का तेजी से आदान-प्रदान होता है। पौधे, एक नियम के रूप में, मुक्त ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, और जानवर श्वसन के माध्यम से इसका उपभोग करते हैं। पृथ्वी पर सबसे व्यापक और गतिशील तत्व होने के नाते, ऑक्सीजन पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व और कार्यों को सीमित नहीं करता है, हालांकि जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता अस्थायी रूप से सीमित हो सकती है। जीवमंडल में ऑक्सीजन चक्र अत्यंत जटिल है, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं। परिणामस्वरूप, कई महाकाव्य चक्र घटित होते हैं, जो स्थलमंडल और वायुमंडल के बीच या जलमंडल और इन दो वातावरणों के बीच घटित होते हैं। ऑक्सीजन चक्र कुछ मायनों में रिवर्स कार्बन डाइऑक्साइड चक्र के समान है। एक की गति दूसरे की गति के विपरीत दिशा में होती है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन की खपत और प्राथमिक उत्पादकों द्वारा इसका प्रतिस्थापन अपेक्षाकृत तेज़ी से होता है। इस प्रकार, सभी वायुमंडलीय ऑक्सीजन को पूरी तरह से नवीनीकृत करने में 2000 वर्ष लगते हैं। आजकल, वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचय नहीं हो पाता है और इसकी मात्रा (20.946%) स्थिर रहती है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में, जब पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन पर कार्य करता है, तो ओजोन - O3 - बनता है। पृथ्वी तक पहुँचने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 5% ओजोन के निर्माण पर खर्च होता है - लगभग 8.6 * 1015 W। प्रतिक्रियाएँ आसानी से प्रतिवर्ती होती हैं। जब ओजोन का क्षय होता है, तो यह ऊर्जा निकलती है, जो ऊपरी वायुमंडल में उच्च तापमान बनाए रखती है। वायुमंडल में औसत ओजोन सांद्रता लगभग 106 वोल्ट है। %; अधिकतम O3 सांद्रता - 4-10 "* वॉल्यूम% तक - 20-25 किमी (टी.ए. अकीमोवा, वी.वी. हास्किन, 1998) की ऊंचाई पर हासिल की जाती है। ओजोन एक प्रकार के यूवी फिल्टर के रूप में कार्य करता है: यह कठोर पराबैंगनी किरणों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रोकता है। संभवतः, ओजोन परत का निर्माण समुद्र से जीवन के उभरने और भूमि पर निवास करने की स्थितियों में से एक था। भूवैज्ञानिक युगों के दौरान उत्पादित अधिकांश ऑक्सीजन वायुमंडल में नहीं रहती थी, बल्कि कार्बोनेट, सल्फेट्स, आयरन ऑक्साइड आदि के रूप में स्थलमंडल द्वारा स्थिर हो जाती थी। यह द्रव्यमान 590 * 1014 टन बनाम 39 * 1014 टन ऑक्सीजन है, जो महाद्वीपीय और समुद्री जल में घुली गैस या सल्फेट्स के रूप में जीवमंडल में घूमता है। नाइट्रोजन चक्र. नाइट्रोजन एक आवश्यक बायोजेनिक तत्व है, क्योंकि यह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा है। नाइट्रोजन चक्र सबसे जटिल में से एक है, क्योंकि इसमें गैस और खनिज दोनों चरण शामिल हैं, और साथ ही सबसे आदर्श चक्र भी शामिल हैं। नाइट्रोजन चक्र का कार्बन चक्र से गहरा संबंध है। एक नियम के रूप में, नाइट्रोजन कार्बन का अनुसरण करती है, जिसके साथ यह सभी प्रोटीन पदार्थों के निर्माण में भाग लेती है। वायुमंडलीय वायु, जिसमें 78% नाइट्रोजन होती है, एक अक्षय भंडार है। हालाँकि, अधिकांश जीवित जीव इस नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। पौधों द्वारा नाइट्रोजन को अवशोषित करने के लिए, इसे अमोनियम (NH*) या नाइट्रेट (NO3) आयनों का हिस्सा होना चाहिए। जीवाणुओं के विनाइट्रीकरण के कार्य के परिणामस्वरूप नाइट्रोजन गैस लगातार वायुमंडल में छोड़ी जाती है, और स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, नीले-हरे शैवाल (साइनोफाइट्स) के साथ मिलकर, इसे लगातार अवशोषित करते हैं, इसे नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। विनाशकों के स्तर पर नाइट्रोजन चक्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पौधों और जानवरों में मौजूद प्रोटीन और कार्बनिक नाइट्रोजन के अन्य रूप उनकी मृत्यु के बाद हेटरोट्रॉफ़िक बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेट्स, कवक (जैव कम करने वाले सूक्ष्मजीव) के संपर्क में आते हैं, जो इस कार्बनिक नाइट्रोजन को कम करके, इसे अमोनिया में परिवर्तित करके आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। मिट्टी में, नाइट्रीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसमें प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल होती है, जहां, सूक्ष्मजीवों की भागीदारी के साथ, अमोनियम आयन (NH4+) का नाइट्राइट (NO~) या नाइट्राइट से नाइट्रेट (N0~) में ऑक्सीकरण होता है। गैसीय यौगिकों आणविक नाइट्रोजन (एन2) या नाइट्रस ऑक्साइड (एन20) में नाइट्राइट और नाइट्रेट की कमी विनाइट्रीकरण प्रक्रिया का सार है। आंधी के दौरान विद्युत निर्वहन के दौरान वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बांधने और फिर बारिश के साथ मिट्टी की सतह पर गिरने से वायुमंडल में छोटी मात्रा में अकार्बनिक रूप से नाइट्रेट का निर्माण लगातार होता रहता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का एक अन्य स्रोत ज्वालामुखी हैं, जो महासागरों के तल में अवसादन या जमाव के दौरान चक्र से बाहर किए गए नाइट्रोजन के नुकसान की भरपाई करते हैं। सामान्य तौर पर, वायुमंडल से मिट्टी में जमाव के दौरान अजैविक मूल के नाइट्रेट नाइट्रोजन की औसत आपूर्ति 10 किलोग्राम (वर्ष/हेक्टेयर) से अधिक नहीं होती है, मुक्त बैक्टीरिया 25 किलोग्राम (वर्ष/हेक्टेयर) का उत्पादन करते हैं, जबकि फलीदार पौधों के साथ राइजोबियम का सहजीवन होता है। औसतन 200 किलोग्राम (वर्ष/हेक्टेयर) उत्पादन होता है। स्थिर नाइट्रोजन का मुख्य भाग जीवाणुओं को एन2 में विनाइट्रिफाई करके संसाधित किया जाता है और वायुमंडल में वापस लौटा दिया जाता है। केवल 10% अमोनीकृत और नाइट्रिफाइड नाइट्रोजन उच्च पौधों द्वारा मिट्टी से अवशोषित किया जाता है और बायोकेनोज़ के बहुकोशिकीय प्रतिनिधियों के निपटान में समाप्त होता है। फास्फोरस चक्र. जीवमंडल में फास्फोरस चक्र पौधों और जानवरों में चयापचय प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। प्रोटोप्लाज्म का यह महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व, स्थलीय पौधों और शैवाल में 0.01-0.1%, जानवरों में 0.1% से कई प्रतिशत तक निहित होता है, घूमता है, धीरे-धीरे कार्बनिक यौगिकों से फॉस्फेट में बदल जाता है, जिसे फिर से पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। हालाँकि, फॉस्फोरस, अन्य बायोफिलिक तत्वों के विपरीत, प्रवास के दौरान गैस का रूप नहीं बनाता है। फास्फोरस का भंडार नाइट्रोजन की तरह वायुमंडल नहीं है, बल्कि स्थलमंडल का खनिज भाग है। अकार्बनिक फास्फोरस के मुख्य स्रोत आग्नेय चट्टानें (एपेटाइट) या तलछटी चट्टानें (फॉस्फोराइट्स) हैं। चट्टानों से, अकार्बनिक फास्फोरस निक्षालन और महाद्वीपीय जल में घुलकर परिसंचरण में शामिल होता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और मिट्टी में जाकर, फॉस्फोरस पौधों द्वारा अकार्बनिक फॉस्फेट आयन के रूप में एक जलीय घोल से अवशोषित किया जाता है और विभिन्न कार्बनिक यौगिकों में शामिल किया जाता है, जहां यह कार्बनिक फॉस्फेट के रूप में प्रकट होता है। फास्फोरस खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से पौधों से पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य जीवों तक पहुंचता है। फॉस्फोरस को बहते पानी द्वारा जलीय पारिस्थितिक तंत्र में ले जाया जाता है। नदियाँ लगातार महासागरों को फॉस्फेट से समृद्ध करती रहती हैं। जहां फास्फोरस फाइटोप्लांकटन का हिस्सा बन जाता है। कुछ फॉस्फोरस यौगिक उथली गहराई में चले जाते हैं और जीवों द्वारा खा लिए जाते हैं, जबकि दूसरा भाग अधिक गहराई में खो जाता है। जीवों के मृत अवशेष विभिन्न गहराईयों पर फास्फोरस के संचय का कारण बनते हैं। सल्फर चक्र. कई गैसीय सल्फर यौगिक हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। हालाँकि, इस तत्व के चक्र का प्रमुख हिस्सा प्रकृति में तलछटी है और मिट्टी और पानी में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में अकार्बनिक सल्फर की उपलब्धता पानी में कई सल्फेट्स की अच्छी घुलनशीलता से सुगम होती है। पौधे, सल्फेट्स को अवशोषित करते हैं, उन्हें कम करते हैं और सल्फर युक्त अमीनो एसिड (मेथिओनिन, सिस्टीन, सिस्टीन) का उत्पादन करते हैं जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के विभिन्न क्षेत्रों के बीच डाइसल्फ़ाइड पुलों के निर्माण के दौरान प्रोटीन की तृतीयक संरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैव-भू-रासायनिक चक्र की कई बुनियादी विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं: एस -> एस -> एसओ2 - रंगहीन, हरा और बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया; - "एच2एस (सल्फेट का अवायवीय अपचयन) - डेसल्फोविबनो; एच2एस - "एसओ2" (सल्फाइड का एरोबिक ऑक्सीकरण) - थायोबैसिलस; एसओ और एच2एस में कार्बनिक एस। - क्रमशः एरोबिक और एनारोबिक हेटरोट्रॉफ़िक सूक्ष्मजीव। प्राथमिक उत्पादन कार्बनिक पदार्थों में सल्फेट के समावेश को सुनिश्चित करता है, और जानवरों द्वारा उत्सर्जन सल्फेट को चक्र में वापस लाने के एक तरीके के रूप में कार्य करता है। सामान्य तौर पर, पारिस्थितिकी तंत्र को नाइट्रोजन और फास्फोरस की तुलना में कम सल्फर की आवश्यकता होती है। इसलिए, सल्फर अक्सर पौधों और जानवरों के लिए एक सीमित कारक नहीं होता है। साथ ही, बायोमास उत्पादन और अपघटन की समग्र प्रक्रिया में सल्फर चक्र महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जब लौह सल्फाइड तलछट में बनता है, तो फॉस्फोरस अघुलनशील रूप से घुलनशील रूप में स्थानांतरित हो जाता है और जीवों के लिए उपलब्ध हो जाता है। यह इस बात की पुष्टि है कि एक चक्र को दूसरे द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाता है। 2 पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह उन पदार्थों के विपरीत जो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न ब्लॉकों के माध्यम से लगातार घूमते रहते हैं, जिन्हें हमेशा पुन: उपयोग किया जा सकता है और चक्र में प्रवेश किया जा सकता है, ऊर्जा का उपयोग एक बार किया जा सकता है, अर्थात। पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा का एक रैखिक प्रवाह होता है। एक सार्वभौमिक प्राकृतिक घटना के रूप में ऊर्जा का एकतरफा प्रवाह थर्मोडायनामिक्स के नियमों के परिणामस्वरूप होता है। पहला नियम कहता है कि ऊर्जा को एक रूप (जैसे प्रकाश) से दूसरे रूप (जैसे भोजन की संभावित ऊर्जा) में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरे नियम में कहा गया है कि ऊर्जा के परिवर्तन से जुड़ी एक भी प्रक्रिया इसका कुछ हिस्सा खोए बिना नहीं हो सकती है। ऐसे परिवर्तनों में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा दुर्गम तापीय ऊर्जा में नष्ट हो जाती है और इसलिए नष्ट हो जाती है। इसलिए: उदाहरण के लिए, खाद्य पदार्थों का जीव के शरीर को बनाने वाले पदार्थ में 100% दक्षता के साथ परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस प्रकार, जीवित जीव ऊर्जा परिवर्तक हैं। और हर बार जब ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो इसका कुछ हिस्सा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाता है। अंततः, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक चक्र में प्रवेश करने वाली सारी ऊर्जा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है। जीवित जीव वास्तव में काम करने के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में गर्मी का उपयोग नहीं करते हैं - वे प्रकाश और रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं और नेटवर्क, पोषी स्तर। एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर, ऊर्जा युक्त पदार्थ स्वपोषी जीवों द्वारा बनाए जाते हैं और विषमपोषी जीवों के लिए भोजन के रूप में काम करते हैं। खाद्य कनेक्शन एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा स्थानांतरित करने के तंत्र हैं। एक विशिष्ट उदाहरण: एक जानवर पौधे खाता है। बदले में, इस जानवर को कोई अन्य जानवर खा सकता है। इस तरह, ऊर्जा को कई जीवों के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है - प्रत्येक बाद वाला पिछले एक पर फ़ीड करता है, जो इसे कच्चे माल और ऊर्जा की आपूर्ति करता है। ऊर्जा स्थानांतरण के इस क्रम को खाद्य (ट्रॉफिक) श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक कड़ी का स्थान एक पोषी स्तर है। पहले पोषी स्तर पर, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, स्वपोषी, या तथाकथित प्राथमिक उत्पादकों का कब्जा है। दूसरे पोषी स्तर के जीवों को प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरे को द्वितीयक उपभोक्ता आदि कहा जाता है। आम तौर पर खाद्य श्रृंखलाएं तीन प्रकार की होती हैं। मांसाहारी खाद्य श्रृंखला पौधों से शुरू होती है और छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर बढ़ती है। भूमि पर, खाद्य श्रृंखलाएँ तीन से चार कड़ियों से बनी होती हैं। सबसे सरल खाद्य श्रृंखलाओं में से एक इस प्रकार दिखती है: पौधा -> खरगोश -> भेड़िया उत्पादक -" शाकाहारी -> -> मांसाहारी निम्नलिखित खाद्य शृंखलाएँ भी व्यापक हैं: पौधे की सामग्री (जैसे अमृत) - "मक्खी -" - "मकड़ी -> छछूंदर -> उल्लू। गुलाब की झाड़ी का रस -> एफिड -> -> लेडीबग -> -> मकड़ी - "कीटभक्षी पक्षी -> शिकार का पक्षी। जलीय और विशेष रूप से समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में, शिकारी खाद्य श्रृंखलाएं स्थलीय की तुलना में लंबी होती हैं। तीसरे प्रकार की खाद्य शृंखलाएँ, जो मृत पौधों के अवशेषों, शवों और जानवरों के मलमूत्र से शुरू होती हैं, डेट्राइटल (सैप्रोफाइटिक) खाद्य श्रृंखलाएँ या डेट्राइटल अपघटन श्रृंखलाएँ कहलाती हैं। पर्णपाती वन स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की व्युत्पन्न खाद्य श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें से अधिकांश पत्ते शाकाहारी जानवरों द्वारा नहीं खाए जाते हैं और गिरी हुई पत्तियों के कूड़े का हिस्सा होते हैं। पत्तियों को कई हानिकारक जीवों - कवक, बैक्टीरिया, कीड़े (उदाहरण के लिए, कोलेम्बोला), आदि द्वारा कुचल दिया जाता है, और फिर केंचुओं द्वारा निगला जाता है, जो पृथ्वी की सतह परत में ह्यूमस को समान रूप से वितरित करते हैं, जिससे तथाकथित मल बनता है। इस स्तर पर, मशरूम में माइसेलियम विकसित होता है। श्रृंखला को पूरा करने वाले विघटित सूक्ष्मजीव मृत कार्बनिक पदार्थों के अंतिम खनिजकरण का उत्पादन करते हैं। सामान्य तौर पर, हमारे वनों की विशिष्ट व्युत्पन्न खाद्य श्रृंखलाओं को निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है: पत्ती कूड़ा -> केंचुआ -> ब्लैकबर्ड - स्पैरोहॉक; मृत जानवर - "कैरियन मक्खियों का लार्वा -" घास मेंढक -> सामान्य घास साँप। चर्चा की गई खाद्य श्रृंखला आरेखों में, प्रत्येक जीव को एक प्रकार के अन्य जीवों पर भोजन करने के रूप में दर्शाया गया है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में वास्तविक खाद्य संबंध बहुत अधिक जटिल होते हैं, क्योंकि एक जानवर एक ही खाद्य श्रृंखला से या विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं से विभिन्न प्रकार के जीवों को खा सकता है, उदाहरण के लिए, ऊपरी पोषी स्तर के शिकारी। जानवर अक्सर पौधों और अन्य जानवरों दोनों को खाते हैं। इन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल बहुत जटिल होते हैं, और हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनमें प्रवेश करने वाली ऊर्जा को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होने में लंबा समय लगता है। पारिस्थितिक पिरामिड. प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर, खाद्य जालों की एक अच्छी तरह से परिभाषित संरचना होती है, जो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के प्रत्येक स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले जीवों की प्रकृति और संख्या की विशेषता होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन करने और उन्हें ग्राफिक रूप से चित्रित करने के लिए, वे आमतौर पर खाद्य वेब आरेखों के बजाय पारिस्थितिक पिरामिड का उपयोग करते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र की पोषी संरचना को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं। इनका निर्माण समान चौड़ाई के आयतों के रूप में किया जाता है, लेकिन आयतों की लंबाई मापी जाने वाली वस्तु के मान के समानुपाती होनी चाहिए। यहां से आप संख्याओं, बायोमास और ऊर्जा के पिरामिड प्राप्त कर सकते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड किसी भी बायोसेनोसिस की मूलभूत विशेषताओं को दर्शाते हैं जब वे इसकी ट्रॉफिक संरचना दिखाते हैं। संख्याओं के पिरामिड. वे किसी पारिस्थितिकी तंत्र की पोषी संरचना के अध्ययन के लिए सबसे सरल सन्निकटन का प्रतिनिधित्व करते हैं। बायोमास पिरामिड. पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण संबंधी संबंधों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि यह प्रत्येक पोषी स्तर के जीवों (बायोमास) के कुल द्रव्यमान को ध्यान में रखता है। ऊर्जा का पिरामिड. विभिन्न पोषी स्तरों पर जीवों के बीच संबंध प्रदर्शित करने का सबसे मौलिक तरीका ऊर्जा पिरामिड के माध्यम से है। वे खाद्य श्रृंखलाओं की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता और उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रति इकाई सतह क्षेत्र में प्रति इकाई समय में संचित ऊर्जा (केकेसी) की मात्रा की गणना करके और प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों द्वारा उपयोग की जाती है। पौधे द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में केवल आंशिक रूप से किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में निर्धारित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के सकल उत्पादन का प्रतिनिधित्व करती है। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग प्रोटोप्लाज्म और पौधों के विकास के लिए किया जाता है। उनकी ऊर्जा का एक हिस्सा सांस लेने पर खर्च होता है। दूसरे दर्जे के उपभोक्ता (शिकारी) अपने पीड़ितों के पूरे बायोमास को नष्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा, जिस मात्रा को वे नष्ट करते हैं, उसका केवल एक हिस्सा ही उनके अपने पोषी स्तर का बायोमास बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बाकी हिस्सा मुख्य रूप से सांस लेने की ऊर्जा पर खर्च होता है और मल-मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। 1942 में, आर. लिंडमैन ने पहली बार ऊर्जा के पिरामिड का नियम तैयार किया, जिसे पाठ्यपुस्तकों में अक्सर "10% का नियम" कहा जाता है। इस नियम के अनुसार, औसतन 10% से अधिक ऊर्जा पारिस्थितिक पिरामिड के एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर तक नहीं जाती है। प्रारंभिक ऊर्जा का केवल 10-20% बाद के हेटरोट्रॉफ़्स में स्थानांतरित किया जाता है। ऊर्जा पिरामिड के नियम का उपयोग करके, यह गणना करना आसान है कि तृतीयक मांसाहारी (ट्रॉफिक स्तर V) तक पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा उत्पादकों द्वारा अवशोषित ऊर्जा का लगभग 0.0001 है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर तक स्थानांतरण बहुत कम दक्षता के साथ होता है। यह किसी विशेष बायोकेनोसिस की परवाह किए बिना, खाद्य श्रृंखला में लिंक की सीमित संख्या की व्याख्या करता है। ई. ओडुम (1959) एक अत्यंत सरलीकृत खाद्य श्रृंखला में - अल्फाल्फा -> बछड़ा - "बच्चे ने ऊर्जा के परिवर्तन का आकलन किया, इसके नुकसान की भयावहता को चित्रित किया। मान लीजिए, उन्होंने तर्क दिया, एक क्षेत्र में अल्फाल्फा की फसलें हैं 4 हेक्टेयर। इस क्षेत्र में बछड़े भोजन करते हैं (यह माना जाता है कि वे केवल अल्फाल्फा खाते हैं), और एक 12 वर्षीय लड़का विशेष रूप से वील खाता है। गणना के परिणाम, तीन पिरामिडों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं: संख्याएं, बायोमास और ऊर्जा, संकेत मिलता है कि अल्फाल्फा क्षेत्र में गिरने वाली सभी सौर ऊर्जा का केवल 0.24% उपयोग करता है; बछड़ा इस उत्पाद का 8% अवशोषित करता है और बछड़े के बायोमास का केवल 0.7% वर्ष के दौरान बच्चे के विकास को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार, ई. ओडुम ने दिखाया कि आपतित सौर ऊर्जा का केवल दस लाखवां हिस्सा ही मांसाहारी बायोमास में परिवर्तित होता है, इस मामले में बच्चे के वजन में वृद्धि में योगदान होता है, और बाकी पर्यावरण में नष्ट हो जाता है और नष्ट हो जाता है। उपरोक्त उदाहरण स्पष्ट रूप से पारिस्थितिक तंत्र की बहुत कम पारिस्थितिक दक्षता और खाद्य श्रृंखलाओं में परिवर्तन की कम दक्षता को दर्शाता है। हम निम्नलिखित बता सकते हैं: यदि 1000 किलो कैलोरी (दिन मी.) 2) उत्पादकों द्वारा दर्ज किया गया, फिर 10 किलो कैलोरी (दिन मी 2) शाकाहारी जीवों के बायोमास में जाता है और केवल 1 किलो कैलोरी (दिन मी.) 2) - मांसाहारियों के बायोमास में। चूँकि किसी पदार्थ की एक निश्चित मात्रा का उपयोग प्रत्येक बायोसेनोसिस द्वारा बार-बार किया जा सकता है, और ऊर्जा का एक हिस्सा एक बार, यह कहना अधिक समीचीन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक कैस्केड स्थानांतरण होता है। उपभोक्ता पारिस्थितिकी तंत्र में प्रबंधन और स्थिरीकरण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। उपभोक्ता प्रभुत्वशाली लोगों के एकाधिकार को रोकते हुए, सेनोसिस में विविधता का एक स्पेक्ट्रम उत्पन्न करते हैं। उपभोक्ताओं के मूल्य को नियंत्रित करने के नियम को उचित रूप से काफी मौलिक माना जा सकता है। साइबरनेटिक विचारों के अनुसार, नियंत्रण प्रणाली की संरचना नियंत्रित प्रणाली से अधिक जटिल होनी चाहिए, तब परिसंपत्तियों के प्रकार की बहुलता का कारण स्पष्ट हो जाता है। उपभोक्ताओं के नियंत्रण महत्व का भी एक ऊर्जावान आधार है। एक या दूसरे पोषी स्तर के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह अंतर्निहित पोषी स्तर में भोजन की उपलब्धता से पूरी तरह से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि ज्ञात है, हमेशा पर्याप्त "भंडार" बचा रहता है, क्योंकि भोजन के पूर्ण विनाश से उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाएगी। ये सामान्य पैटर्न जनसंख्या प्रक्रियाओं, समुदायों, पारिस्थितिक पिरामिड के स्तर और समग्र रूप से बायोकेनोज के ढांचे के भीतर देखे जाते हैं। 3 गतिशील प्रक्रियाएं जो पारिस्थितिक तंत्र में अखंडता और स्थिरता सुनिश्चित करती हैं समुदायों में चक्रीय परिवर्तन बाहरी स्थितियों की दैनिक, मौसमी और दीर्घकालिक आवधिकता और जीवों की अंतर्जात लय की अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की दैनिक गतिशीलता मुख्य रूप से प्राकृतिक घटनाओं की लय से जुड़ी होती है और प्रकृति में सख्ती से आवधिक होती है। हम पहले ही विचार कर चुके हैं कि प्रत्येक बायोकेनोसिस में जीवों के समूह होते हैं जिनकी जीवन गतिविधि दिन के अलग-अलग समय पर होती है। कुछ दिन के दौरान सक्रिय होते हैं, कुछ रात में। इसलिए, किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के व्यक्तिगत प्रकार के बायोकेनोसिस की संरचना और अनुपात में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत जीव एक निश्चित समय के लिए इससे अलग हो जाते हैं। बायोकेनोसिस की दैनिक गतिशीलता जानवरों और पौधों दोनों द्वारा प्रदान की जाती है। जैसा कि ज्ञात है, पौधों में शारीरिक प्रक्रियाओं की तीव्रता और प्रकृति दिन के दौरान बदलती है - प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं होता है, अक्सर पौधों में फूल केवल रात में ही खुलते हैं और रात्रिचर जानवरों द्वारा परागित होते हैं, अन्य दिन के दौरान परागण के लिए अनुकूलित होते हैं। बायोकेनोज़ में दैनिक गतिशीलता, एक नियम के रूप में, अधिक स्पष्ट होती है, दिन और रात के बीच तापमान, आर्द्रता और अन्य पर्यावरणीय कारकों में अंतर जितना अधिक होता है। मौसमी गतिशीलता के साथ बायोकेनोज़ में अधिक महत्वपूर्ण विचलन देखे जाते हैं। यह जीवों के जैविक चक्रों के कारण होता है, जो प्राकृतिक घटनाओं की मौसमी चक्रीयता पर निर्भर करता है। इस प्रकार, मौसम में बदलाव का जानवरों और पौधों की जीवन गतिविधि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है (जानवरों में हाइबरनेशन, सर्दियों की नींद, डायपॉज और प्रवासन; फूलों की अवधि, फलने, सक्रिय विकास, पत्ती गिरने और पौधों में सर्दियों की सुस्ती)। बायोसेनोसिस की स्तरीय संरचना अक्सर मौसमी परिवर्तनशीलता के अधीन होती है। वर्ष के उपयुक्त मौसमों में पौधों की अलग-अलग परतें पूरी तरह से गायब हो सकती हैं, उदाहरण के लिए, वार्षिक पौधों वाली एक जड़ी-बूटी परत। जैविक ऋतुओं की अवधि विभिन्न अक्षांशों पर भिन्न-भिन्न होती है। इस संबंध में, आर्कटिक, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बायोकेनोज़ की मौसमी गतिशीलता अलग-अलग है। यह समशीतोष्ण जलवायु पारिस्थितिकी प्रणालियों और उत्तरी अक्षांशों में सबसे स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। किसी भी बायोकेनोसिस के जीवन में दीर्घकालिक परिवर्तनशीलता सामान्य है। इस प्रकार, बरबिंस्क वन-स्टेप में गिरने वाली वर्षा की मात्रा में साल-दर-साल तेजी से उतार-चढ़ाव होता है; कई शुष्क वर्ष प्रचुर मात्रा में वर्षा की लंबी अवधि के साथ वैकल्पिक होते हैं। इसका पौधों और जानवरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस मामले में, पारिस्थितिक निचे का विकास होता है - उभरते सेट में कार्यात्मक सीमांकन या थोड़ी विविधता के साथ इसका जोड़। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण में आवधिक परिवर्तनों के संबंध में बायोकेनोज़ की संरचना में दीर्घकालिक परिवर्तन भी दोहराए जाते हैं, जो बदले में सौर गतिविधि में वृद्धि या कमी के कारण होता है। दैनिक और मौसमी गतिशीलता की प्रक्रिया में, बायोकेनोज़ की अखंडता का आमतौर पर उल्लंघन नहीं होता है। बायोकेनोसिस गुणात्मक और मात्रात्मक विशेषताओं में केवल आवधिक उतार-चढ़ाव का अनुभव करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रगतिशील परिवर्तन अंततः प्रमुख प्रजातियों के एक अलग समूह के साथ, एक बायोकेनोसिस को दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित करने की ओर ले जाते हैं। ऐसे परिवर्तनों के कारण बायोसेनोसिस के बाहरी कारक हो सकते हैं जो लंबे समय तक एक ही दिशा में कार्य करते हैं, उदाहरण के लिए, जल निकायों का बढ़ता प्रदूषण, पुनर्ग्रहण के परिणामस्वरूप दलदली मिट्टी का सूखना, चराई में वृद्धि आदि। एक बायोकेनोसिस से दूसरे बायोकेनोसिस में होने वाले इन परिवर्तनों को एक्सोजेनेटिक कहा जाता है। ऐसे मामले में जब किसी कारक के बढ़ते प्रभाव से बायोकेनोसिस की संरचना का क्रमिक सरलीकरण होता है, उनकी संरचना में कमी आती है और उत्पादकता में कमी आती है, तो ऐसे बदलावों को डिग्रेसिव या डिग्रेसिव कहा जाता है। बायोकेनोसिस के भीतर होने वाली प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप अंतर्जात परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। एक बायोसेनोसिस के दूसरे द्वारा क्रमिक प्रतिस्थापन को पारिस्थितिक उत्तराधिकार कहा जाता है (अक्षांश से - उत्तराधिकार - अनुक्रम, परिवर्तन)। उत्तराधिकार पारिस्थितिक तंत्र के आत्म-विकास की एक प्रक्रिया है। उत्तराधिकार किसी दिए गए बायोसेनोसिस में जैविक चक्र की अपूर्णता पर आधारित है। यह ज्ञात है कि जीवित जीव, अपनी महत्वपूर्ण गतिविधि के परिणामस्वरूप, अपने आस-पास के वातावरण को बदलते हैं, इसमें से कुछ पदार्थों को निकालते हैं और इसे चयापचय उत्पादों से संतृप्त करते हैं। जब आबादी अपेक्षाकृत लंबे समय तक मौजूद रहती है, तो वे अपने पर्यावरण को प्रतिकूल दिशा में बदल देती हैं और परिणामस्वरूप, खुद को अन्य प्रजातियों की आबादी से विस्थापित पाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तन पारिस्थितिक रूप से फायदेमंद साबित होते हैं। बायोसेनोसिस में, इस प्रकार प्रमुख प्रजातियों में परिवर्तन होता है। पारिस्थितिक दोहराव का नियम (सिद्धांत) यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बायोकेनोसिस का दीर्घकालिक अस्तित्व तभी संभव है जब कुछ जीवित जीवों की गतिविधि के कारण पर्यावरण में परिवर्तन विपरीत आवश्यकताओं वाले अन्य जीवों के लिए अनुकूल हो। उत्तराधिकार के दौरान प्रजातियों की प्रतिस्पर्धी अंतःक्रियाओं के आधार पर, धीरे-धीरे अधिक स्थिर संयोजन बनते हैं जो विशिष्ट अजैविक पर्यावरणीय स्थितियों के अनुरूप होते हैं। एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन की ओर ले जाने वाले उत्तराधिकार का एक उदाहरण एक छोटी झील का अत्यधिक बढ़ना, उसके बाद एक दलदल और फिर उसके स्थान पर एक जंगल का प्रकट होना है। सबसे पहले, झील के किनारों पर एक तैरता हुआ कालीन बनता है - सेज, काई और अन्य पौधों का एक तैरता हुआ कालीन। झील लगातार मृत पौधों के अवशेषों - पीट से भरी रहती है। एक दलदल बनता है, जो धीरे-धीरे जंगल से घिर जाता है। समुदायों की एक क्रमिक श्रृंखला जो धीरे-धीरे और स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे को उत्तराधिकार में प्रतिस्थापित करती है, उत्तराधिकार श्रृंखला कहलाती है। प्रकृति में उत्तराधिकार के पैमाने अत्यंत विविध होते हैं। उन्हें संस्कृतियों वाले बैंकों में देखा जा सकता है, जो प्लवक समुदाय हैं - विभिन्न प्रकार के तैरते शैवाल और उनके उपभोक्ता - रोटिफ़र्स, पोखरों और तालाबों में फ्लैगेलेट्स, दलदल, घास के मैदान, जंगल, परित्यक्त कृषि योग्य भूमि, अपक्षयित चट्टानें, आदि। एक पदानुक्रम है पारिस्थितिक तंत्र के संगठन में यह उत्तराधिकार प्रक्रियाओं में भी प्रकट होता है - बायोकेनोज के बड़े परिवर्तन छोटे से बने होते हैं। पदार्थों के एक विनियमित चक्र के साथ स्थिर पारिस्थितिक तंत्र में, स्थानीय क्रमिक परिवर्तन भी लगातार हो रहे हैं, जो समुदायों की जटिल आंतरिक संरचना का समर्थन करते हैं। क्रमिक परिवर्तनों के प्रकार. क्रमिक परिवर्तन के दो मुख्य प्रकार हैं: 1 - ऑटोट्रॉफ़िक और हेटरोट्रॉफ़िक आबादी की भागीदारी के साथ; 2 - केवल हेटरोट्रॉफ़्स की भागीदारी के साथ। दूसरे प्रकार का उत्तराधिकार केवल उन स्थितियों में होता है जहां कार्बनिक यौगिकों की प्रारंभिक आपूर्ति या निरंतर आपूर्ति बनाई जाती है, जिसके कारण समुदाय मौजूद होता है: खाद के ढेर या ढेर में, विघटित पौधों के पदार्थ में, कार्बनिक पदार्थों से प्रदूषित जलाशयों में, आदि। उत्तराधिकार प्रक्रिया. एफ. क्लेमेंट्स (1916) के अनुसार, उत्तराधिकार की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं: वनस्पति परिवर्तन के साथ उत्तराधिकार प्राथमिक और द्वितीयक हो सकता है। प्राथमिक उत्तराधिकार पहले से निर्जन क्षेत्रों में पारिस्थितिक तंत्र के विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया है, जो उनके उपनिवेशण से शुरू होती है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण नंगी चट्टानों का लगातार गंदा होना और अंततः उन पर वनों का विकास है। इस प्रकार, यूराल पर्वत की चट्टानों पर होने वाले प्राथमिक अनुक्रमों में, निम्नलिखित चरण प्रतिष्ठित हैं: द्वितीयक उत्तराधिकार एक पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली है जो एक बार किसी दिए गए क्षेत्र में मौजूद था। इसकी शुरुआत तब होती है जब ज्वालामुखी विस्फोट, आग, कटाई, जुताई आदि के परिणामस्वरूप स्थापित बायोकेनोसिस में जीवों के स्थापित रिश्ते बाधित हो जाते हैं। पिछले बायोकेनोसिस की बहाली की ओर ले जाने वाले बदलावों को जियोबॉटनी में डिम्यूटेशनल कहा जाता है। एक उदाहरण ज्वालामुखी द्वारा देशी वनस्पतियों और जीवों के पूर्ण विनाश के बाद क्राकाटोआ द्वीप पर प्रजातियों की विविधता की गतिशीलता है। एक अन्य उदाहरण विनाशकारी जंगल की आग के बाद साइबेरियाई अंधेरे शंकुधारी जंगल (फ़िर-देवदार टैगा) का द्वितीयक उत्तराधिकार है। अधिक झुलसे हुए क्षेत्रों में, अग्रणी काई हवा से उड़ने वाले बीजाणुओं से प्रकट होती है: आग लगने के 3-5 साल बाद, सबसे प्रचुर मात्रा में "फायर मॉस" फनारिया हाइग्रोमेट्रिका, गेराटोडोन पुरप्यूरियस आदि हैं। उच्च पौधों में, फायरवीड (चामेनेरियन एंगुस्टिफोलियम) बहुत तेजी से बढ़ता है। जले हुए क्षेत्रों पर उपनिवेश स्थापित करता है), जो पहले से ही 2-3 महीनों के बाद आग में प्रचुर मात्रा में खिलता है, साथ ही जमीन ईख घास (कैलामाग्रोस्टिस एपिगियोस) और अन्य प्रजातियां। आगे उत्तराधिकार के चरण देखे गए हैं: ईख घास का मैदान झाड़ियों को रास्ता देता है, फिर बर्च या एस्पेन वन, मिश्रित देवदार-पत्ते वाले जंगल, देवदार के जंगल, देवदार-देवदार के जंगल, और अंत में, 250 वर्षों के बाद, देवदार-देवदार के जंगल की बहाली होती है . द्वितीयक उत्तराधिकार, एक नियम के रूप में, प्राथमिक उत्तराधिकारियों की तुलना में तेजी से और आसानी से घटित होते हैं, क्योंकि अशांत निवास स्थान में मिट्टी की रूपरेखा, बीज, प्राइमर्डिया और पिछली आबादी का हिस्सा और पिछले कनेक्शन संरक्षित होते हैं। पदावनति प्राथमिक उत्तराधिकार के किसी भी चरण की पुनरावृत्ति नहीं है। चरमोत्कर्ष पारिस्थितिकी तंत्र. उत्तराधिकार एक ऐसे चरण के साथ समाप्त होता है जब पारिस्थितिकी तंत्र की सभी प्रजातियां, प्रजनन करते समय, अपेक्षाकृत स्थिर संख्या बनाए रखती हैं और इसकी संरचना में कोई और परिवर्तन नहीं होता है। इस संतुलन अवस्था को चरमोत्कर्ष कहा जाता है, और पारिस्थितिकी तंत्र को चरमोत्कर्ष कहा जाता है। विभिन्न अजैविक परिस्थितियों में, विभिन्न चरम पारिस्थितिकी तंत्र बनते हैं। गर्म और आर्द्र जलवायु में यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन होगा, शुष्क और गर्म जलवायु में यह रेगिस्तान होगा। पृथ्वी के मुख्य बायोम अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों के चरम पारिस्थितिकी तंत्र हैं। उत्तराधिकार के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन। उत्पादकता और बायोमास. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, उत्तराधिकार एक प्राकृतिक, निर्देशित प्रक्रिया है और एक या दूसरे चरण में होने वाले परिवर्तन किसी भी समुदाय की विशेषता होते हैं और इसकी प्रजाति संरचना या भौगोलिक स्थिति पर निर्भर नहीं होते हैं। क्रमिक परिवर्तन के चार मुख्य प्रकार हैं: यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्तराधिकार चरणों का परिवर्तन कुछ नियमों के अनुसार होता है। प्रत्येक चरण अगले चरण के उद्भव के लिए वातावरण तैयार करता है। विकास के चरणों के पारित होने के क्रम का नियम यहां संचालित होता है; एक प्राकृतिक प्रणाली के विकास के चरण केवल विकासात्मक रूप से निश्चित (ऐतिहासिक, पर्यावरणीय रूप से निर्धारित) क्रम में चल सकते हैं, आमतौर पर अपेक्षाकृत सरल से जटिल तक, एक नियम के रूप में, बिना नुकसान के मध्यवर्ती चरणों के, लेकिन संभवतः उनके बहुत तेजी से पारित होने या विकासात्मक रूप से निश्चित अनुपस्थिति के साथ। जब कोई पारिस्थितिकी तंत्र रजोनिवृत्ति की स्थिति में पहुंचता है, तो उसमें, सभी संतुलन प्रणालियों की तरह, सभी विकास प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं। यह स्थिति क्रमिक मंदी के नियम में परिलक्षित होती है: परिपक्व संतुलन पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाली प्रक्रियाएं जो एक स्थिर स्थिति में होती हैं, एक नियम के रूप में धीमी हो जाती हैं। इस मामले में, उत्तराधिकार का पुनर्स्थापनात्मक प्रकार उनके धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम में बदल जाता है, अर्थात। आत्म-विकास रजोनिवृत्ति या नोडल विकास की सीमा के भीतर होता है। क्रमिक मंदी का अनुभवजन्य नियम जी. ओडुम और आर. पिंकर्टन के नियम या एक परिपक्व प्रणाली को बनाए रखने के लिए अधिकतम ऊर्जा के नियम का परिणाम है: उत्तराधिकार ऊर्जा के प्रवाह में मौलिक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ता है। मात्रा, जिसका उद्देश्य सिस्टम को बनाए रखना है। जी. ओडुम और आर. पिंकर्टन का नियम, बदले में, ए. लोटका द्वारा तैयार जैविक प्रणालियों में अधिकतम ऊर्जा के नियम पर आधारित है। इस प्रश्न को बाद में आर. मार्गालेफ़, वाई. ओडुम द्वारा अच्छी तरह से विकसित किया गया था और इसे "शून्य अधिकतम" के सिद्धांत के प्रमाण के रूप में जाना जाता है, या एक परिपक्व पारिस्थितिकी तंत्र में विकास को कम करना: क्रमिक विकास में एक पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा बायोमास बनाता है। न्यूनतम जैविक उत्पादकता. लिंडमैन (1942) ने प्रयोगात्मक रूप से साबित किया कि उत्तराधिकार चरमोत्कर्ष समुदाय तक उत्पादकता में वृद्धि के साथ होता है, जिसमें ऊर्जा रूपांतरण सबसे कुशलता से होता है। ओक और ओक-राख वनों के उत्तराधिकार के अध्ययन के आंकड़ों से पता चलता है कि बाद के चरणों में उनकी उत्पादकता वास्तव में बढ़ जाती है। हालाँकि, चरमोत्कर्ष समुदाय में संक्रमण के दौरान, आमतौर पर समग्र उत्पादकता में कमी होती है। इस प्रकार, पुराने जंगलों में उत्पादकता युवा जंगलों की तुलना में कम है, जो बदले में उनके पूर्ववर्ती अधिक प्रजाति-समृद्ध जड़ी-बूटियों की परतों की तुलना में कम उत्पादक हो सकती है। कुछ जलीय प्रणालियों में उत्पादकता में इसी तरह की गिरावट देखी गई है। इसके अनेक कारण हैं। उनमें से एक यह है कि बढ़ते वन बायोमास में पोषक तत्वों के संचय से उनके चक्रण में कमी आ सकती है। समग्र उत्पादकता में गिरावट केवल व्यक्तियों की जीवन शक्ति में कमी का परिणाम हो सकती है क्योंकि समुदाय में उनकी औसत आयु बढ़ती है। जैसे-जैसे अनुक्रम बढ़ता है, उपलब्ध पोषक तत्वों का बढ़ता अनुपात समुदाय के बायोमास में जमा होता है, और तदनुसार पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक (मिट्टी या पानी में) में उनकी सामग्री कम हो जाती है। उत्पादित मलबे की मात्रा भी बढ़ जाती है। मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी नहीं, बल्कि अपघटक जीव हैं। तदनुरूप परिवर्तन पोषी नेटवर्क में भी होते हैं। डेट्राइटस पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत बन जाता है। अनुक्रमण के दौरान, पदार्थों के जैव-भू-रासायनिक चक्रों की बंदता बढ़ जाती है। वनस्पति आवरण की बहाली शुरू होने के लगभग 10 साल बाद, चक्रों का खुलापन 100 से घटकर 10% हो जाता है, और फिर यह और भी कम हो जाता है, चरमोत्कर्ष चरण में न्यूनतम तक पहुँच जाता है। उत्तराधिकार के दौरान पदार्थों के जैव-रासायनिक चक्र की बढ़ती बंदता का नियम, यह पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है, सामान्य रूप से वनस्पति और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के मानवजनित परिवर्तन द्वारा उल्लंघन किया जाता है। निस्संदेह, इससे जीवमंडल और उसके विभाजनों में विसंगतियों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती है। रजोनिवृत्ति के दौरान प्रजातियों की विविधता में कमी का मतलब इसका कम पारिस्थितिक महत्व नहीं है। प्रजातियों की विविधता उत्तराधिकार, उसकी दिशा को आकार देती है और यह सुनिश्चित करती है कि वास्तविक स्थान जीवन से भरा हो। परिसर को बनाने वाली प्रजातियों की अपर्याप्त संख्या एक उत्तराधिकार श्रृंखला नहीं बना सकती है, और धीरे-धीरे, चरम पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश के साथ, ग्रह का पूर्ण मरुस्थलीकरण होगा। विविधता का मूल्य स्थिर और गतिशील दोनों तरह से कार्यात्मक है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां प्रजातियों की विविधता जीवमंडल के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है, जो उत्तराधिकार प्रक्रिया के सामान्य प्राकृतिक पाठ्यक्रम के आधार के रूप में कार्य करती है, और पर्यावरण स्वयं तेजी से परेशान होता है, उत्तराधिकार चरम चरण तक नहीं पहुंचता है, लेकिन एक नोडल समुदाय के साथ समाप्त होता है - एक पैराक्लाइमैक्स, एक दीर्घकालिक या अल्पकालिक व्युत्पन्न समुदाय। किसी विशेष स्थान के पर्यावरण में गड़बड़ी जितनी गहरी होती है, उत्तराधिकार के पहले चरण समाप्त हो जाते हैं। जब प्रजातियों का एक या समूह उनके विनाश (आवासों का मानवजनित गायब होना, कम अक्सर विलुप्त होना) के परिणामस्वरूप खो जाता है, तो रजोनिवृत्ति की उपलब्धि प्राकृतिक पर्यावरण की पूर्ण बहाली नहीं है। वास्तव में, यह एक नया पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि इसमें नए कनेक्शन उत्पन्न हुए हैं, कई पुराने खो गए हैं, और प्रजातियों का एक अलग "भंग" विकसित हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि खोई हुई प्रजाति को बहाल नहीं किया जा सकता है। जब कोई अजैविक या जैविक कारक बदलता है, उदाहरण के लिए, निरंतर शीतलन के साथ, या एक नई प्रजाति की शुरूआत के साथ, एक प्रजाति जो नई स्थितियों के लिए खराब रूप से अनुकूलित होती है, उसे तीन रास्तों में से एक का सामना करना पड़ेगा। विकासवादी-पारिस्थितिकी अपरिवर्तनीयता का नियम बताता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र जिसने पारिस्थितिक घटकों के असंतुलन के परिणामस्वरूप अपने कुछ तत्वों को खो दिया है या दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, उत्तराधिकार के दौरान अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आ सकता है, यदि परिवर्तनों के दौरान, विकासवादी (सूक्ष्मविकासवादी) ) पारिस्थितिक तत्वों (संरक्षित या अस्थायी रूप से खोए हुए) में परिवर्तन हुए हैं। ऐसे मामले में जब कुछ प्रजातियां उत्तराधिकार के मध्यवर्ती चरणों में खो जाती हैं, तो इस नुकसान की कार्यात्मक रूप से भरपाई की जा सकती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जब विविधता एक महत्वपूर्ण स्तर से अधिक कम हो जाती है, तो उत्तराधिकार का मार्ग विकृत हो जाता है, और वास्तव में, अतीत के समान चरमोत्कर्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पुनर्स्थापित पारिस्थितिक तंत्र की प्रकृति का आकलन करने के लिए, विकासवादी-पारिस्थितिक अपरिवर्तनीयता का नियम महत्वपूर्ण है। तत्वों के नुकसान के साथ, ये वास्तव में, नवगठित पैटर्न और कनेक्शन के साथ पूरी तरह से नए पारिस्थितिक प्राकृतिक निर्माण हैं। इस प्रकार, किसी ऐसी प्रजाति के अतीत में स्थानांतरण जो उसके पुन: अनुकूलन के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र से बाहर हो गई, उसका मतलब उसकी यांत्रिक वापसी नहीं है। यह वास्तव में एक नवीनीकृत पारिस्थितिकी तंत्र में एक नई प्रजाति का परिचय है। विकासवादी-पारिस्थितिक अपरिवर्तनीयता का नियम न केवल बायोसिस्टम के स्तर पर, बल्कि बायोटा के अन्य सभी पदानुक्रमित स्तरों पर भी विकास की दिशा पर जोर देता है। 4 एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जीवमंडल जो पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता और स्थिरता सुनिश्चित करता है जीवमंडल एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जीवमंडल को जियोबायोस्फीयर, हाइड्रोबायोस्फीयर और एरोबायोस्फीयर में विभाजित किया गया है (चित्र 2.4)। जियोबायोस्फीयर में मुख्य पर्यावरण-निर्माण कारकों के अनुसार विभाजन होते हैं: टेराबायोस्फीयर और लिथोबायोस्फीयर - जियोबायोस्फीयर के भीतर, मैरिनोबायोस्फीयर (महासागरीय बायोस्फीयर) और एक्वाबायोस्फीयर - हाइड्रोबायोस्फीयर के भीतर। इन संरचनाओं को उपमंडल कहा जाता है। उनके गठन में अग्रणी पर्यावरण-निर्माण कारक जीवित पर्यावरण का भौतिक चरण है: एरोबायोस्फीयर में हवा-पानी, जल-हाइड्रोबायोस्फीयर में मीठे पानी और खारे पानी, टेराबायोस्फीयर में ठोस-वायु और लिथोबायोस्फीयर में ठोस पानी। बदले में, वे सभी परतों में गिर जाते हैं: एरोबायोस्फीयर - ट्रोपोबायोस्फीयर और एल्टोबायोस्फीयर में; हाइड्रोबायोस्फीयर - प्रकाशमंडल, डिसफोटोस्फीयर और एफोफोटोस्फीयर में। यहाँ संरचना-निर्माण कारक, भौतिक पर्यावरण, ऊर्जा (प्रकाश और गर्मी) के अलावा, जीवन के निर्माण और विकास के लिए विशेष स्थितियाँ - भूमि पर, उसकी गहराई में, ऊपर के स्थानों में बायोटा के प्रवेश की विकासवादी दिशाएँ हैं। पृथ्वी, समुद्र की गहराई, निस्संदेह भिन्न हैं। एपोबायोस्फीयर, पैराबायोस्फीयर और अन्य उप- और सुप्रा-बायोस्फीयर परतों के साथ मिलकर, वे मेगाबायोस्फीयर की सीमाओं के भीतर तथाकथित "जीवन की परत केक" और इसके अस्तित्व के जियोस्फीयर (पारिस्थितिकीमंडल) का गठन करते हैं। एक प्रणालीगत अर्थ में, सूचीबद्ध संरचनाएँ वस्तुतः सार्वभौमिक या उपग्रहीय आयामों के बड़े कार्यात्मक भाग हैं। वैज्ञानिकों का मानना \u200b\u200bहै कि जीवमंडल में 7 मुख्य सामग्री-ऊर्जा पारिस्थितिक घटकों और 8 वें - सूचनात्मक के अंतर्संबंध के भीतर पदार्थों के अपेक्षाकृत स्वतंत्र चक्रों के कम से कम 8-9 स्तर हैं। पदार्थों के वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय चक्र बंद नहीं होते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र पदानुक्रम के भीतर आंशिक रूप से "प्रतिच्छेद" करते हैं। यह सामग्री-ऊर्जा, और आंशिक रूप से सूचनात्मक "युग्मन" समग्र रूप से जीवमंडल तक पारिस्थितिक सुपरसिस्टम की अखंडता सुनिश्चित करता है। पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता और स्थिरता। जीवमंडल का निर्माण काफी हद तक बाहरी कारकों से नहीं, बल्कि आंतरिक पैटर्न से होता है। जीवमंडल की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति जीवित और निर्जीव चीजों की परस्पर क्रिया है, जो वी. आई. वर्नाडस्की द्वारा परमाणुओं के बायोजेनिक प्रवासन के कानून में परिलक्षित होती है। परमाणुओं के बायोजेनिक प्रवासन का नियम मानवता के लिए संपूर्ण पृथ्वी और इसके क्षेत्रों में जैव-भू-रासायनिक प्रक्रियाओं को सचेत रूप से नियंत्रित करना संभव बनाता है। जीवमंडल में जीवित पदार्थ की मात्रा, जैसा कि ज्ञात है, ध्यान देने योग्य परिवर्तनों के अधीन नहीं है। यह पैटर्न वी.आई. द्वारा जीवित पदार्थ की मात्रा की स्थिरता के नियम के रूप में तैयार किया गया था। वर्नाडस्की: किसी दिए गए भूवैज्ञानिक अवधि के लिए जीवमंडल में जीवित पदार्थ की मात्रा एक स्थिर है। व्यवहार में, यह कानून वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र - जीवमंडल के लिए आंतरिक गतिशील संतुलन के कानून का एक मात्रात्मक परिणाम है। चूँकि जीवित पदार्थ, परमाणुओं के बायोजेनिक प्रवासन के नियम के अनुसार, सूर्य और पृथ्वी के बीच एक ऊर्जा मध्यस्थ है, इसकी मात्रा या तो स्थिर होनी चाहिए, या इसकी ऊर्जा विशेषताएँ बदलनी चाहिए। जीवित पदार्थ की भौतिक और रासायनिक एकता का नियम (पृथ्वी के सभी जीवित पदार्थ भौतिक और रासायनिक रूप से एकजुट हैं और बाद की संपत्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को शामिल नहीं करते हैं। इसलिए, ग्रह के जीवित पदार्थ के लिए मात्रात्मक स्थिरता अपरिहार्य है। यह पूरी तरह से विशेषता है) प्रजातियों की संख्या. जीवित पदार्थ, सौर ऊर्जा के संचायक के रूप में, बाहरी (ब्रह्मांडीय) प्रभावों और आंतरिक परिवर्तनों दोनों पर एक साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए। जीवमंडल के एक स्थान पर जीवित पदार्थ की मात्रा में कमी या वृद्धि से दूसरे स्थान पर बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि जारी पोषक तत्वों को शेष जीवित पदार्थ द्वारा आत्मसात किया जा सकता है या उनकी कमी देखी जाएगी। यहां हमें प्रक्रिया की गति को ध्यान में रखना चाहिए, जो मानवजनित परिवर्तन के मामले में मनुष्य द्वारा प्रकृति में प्रत्यक्ष गड़बड़ी की तुलना में बहुत कम है। जीवित पदार्थ की मात्रा की स्थिरता और निरंतरता के अलावा, जो जीवित पदार्थ की भौतिक और रासायनिक एकता के नियम में परिलक्षित होता है, जीवित प्रकृति में सूचनात्मक और दैहिक संरचना का निरंतर संरक्षण होता है, इस तथ्य के बावजूद कि यह बदलता है कुछ हद तक विकास के क्रम के साथ। इस संपत्ति को यू. गोल्डस्मिथ (1981) द्वारा नोट किया गया था और इसे जीवमंडल की संरचना के संरक्षण का कानून कहा गया था - सूचनात्मक और दैहिक, या इकोडायनामिक्स का पहला कानून। जीवमंडल की संरचना को संरक्षित करने के लिए, जीवित चीजें परिपक्वता या पारिस्थितिक संतुलन की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। रजोनिवृत्ति की इच्छा का नियम - यू. गोल्डस्मिथ द्वारा इकोडायनामिक्स का दूसरा नियम, जीवमंडल और पारिस्थितिक प्रणालियों के अन्य स्तरों पर लागू होता है, हालांकि विशिष्टताएं हैं - जीवमंडल अपने उपखंडों की तुलना में अधिक बंद प्रणाली है। जीवमंडल के जीवित पदार्थ की एकता और इसके उपप्रणालियों की संरचना की समरूपता इस तथ्य की ओर ले जाती है कि विभिन्न भूवैज्ञानिक युगों और उस पर उत्पन्न मूल भौगोलिक उत्पत्ति के जीवित तत्व जटिल रूप से विकासात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के सभी पारिस्थितिक स्तरों पर विभिन्न अनुपात-लौकिक उत्पत्ति के तत्वों का अंतर्संबंध जीवित पदार्थ के विषमजनन के नियम या सिद्धांत को दर्शाता है। यह जोड़ अराजक नहीं है, बल्कि पारिस्थितिक संपूरकता, पारिस्थितिक अनुरूपता (अनुरूपता) और अन्य कानूनों के सिद्धांतों के अधीन है। यू. गोल्डस्मिथ के इकोडायनामिक्स के ढांचे के भीतर, यह इसका तीसरा नियम है - पारिस्थितिक क्रम, या पारिस्थितिक पारस्परिकता का सिद्धांत, इसके भागों पर संपूर्ण के प्रभाव के कारण एक वैश्विक संपत्ति का संकेत देता है, विभेदित भागों का विपरीत प्रभाव। संपूर्ण का विकास, आदि, जो समग्र रूप से जीवमंडल के संरक्षण स्थिरता की ओर ले जाता है। पारिस्थितिक व्यवस्था, या प्रणालीगत पारस्परिकता के ढांचे के भीतर पारस्परिक सहायता, स्थान और स्थानिक-लौकिक निश्चितता को भरने के क्रम के कानून द्वारा पुष्टि की जाती है: एक प्राकृतिक प्रणाली के भीतर स्थान को भरने, इसके उप-प्रणालियों के बीच बातचीत के कारण, आदेश दिया जाता है ऐसा तरीका जो सिस्टम के होमोस्टैटिक गुणों को इसके भीतर के हिस्सों के बीच न्यूनतम विरोधाभासों के साथ महसूस करने की अनुमति देता है। इस कानून से यह पता चलता है कि प्रकृति के लिए "अनावश्यक" दुर्घटनाओं का दीर्घकालिक अस्तित्व, जिसमें इसके लिए विदेशी मानव रचनाएँ भी शामिल हैं, असंभव है। जीवमंडल में पारस्परिक प्रणाली क्रम के नियमों में सिस्टम संपूरकता का सिद्धांत भी शामिल है, जो बताता है कि एक प्राकृतिक प्रणाली की उप प्रणालियाँ अपने विकास में उसी प्रणाली में शामिल अन्य उप प्रणालियों के सफल विकास और आत्म-नियमन के लिए एक शर्त प्रदान करती हैं। यू. गोल्डस्मिथ द्वारा इकोडायनामिक्स के चौथे नियम में जीवित चीजों के आत्म-नियंत्रण और आत्म-नियमन का कानून शामिल है: जीवित चीजों के नियंत्रित प्रभाव के तहत जीवित प्रणालियाँ और प्रणालियाँ अपनी प्रक्रिया में आत्म-नियंत्रण और आत्म-नियमन करने में सक्षम हैं। पर्यावरण में परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन। जीवमंडल में, आत्म-नियंत्रण और आत्म-नियमन सामान्य बातचीत के कैस्केड और श्रृंखला प्रक्रियाओं के दौरान होता है - प्राकृतिक चयन के अस्तित्व के लिए संघर्ष के दौरान (इस अवधारणा के व्यापक अर्थ में), सिस्टम और उप-प्रणालियों का अनुकूलन, व्यापक सह-विकास , वगैरह। इसके अलावा, ये सभी प्रक्रियाएं प्रकृति के "दृष्टिकोण से" सकारात्मक परिणाम देती हैं - जीवमंडल और समग्र रूप से पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण और विकास। संरचनात्मक और विकासवादी प्रकृति के सामान्यीकरण के बीच जोड़ने वाली कड़ी वैश्विक आवास के स्वचालित रखरखाव का नियम है: जीवित पदार्थ, स्व-नियमन और अजैविक कारकों के साथ बातचीत के दौरान, अपने विकास के लिए उपयुक्त जीवन वातावरण को स्वचालित रूप से बनाए रखता है। यह प्रक्रिया ब्रह्मांडीय और वैश्विक पारिस्थितिकीय पैमाने में परिवर्तन से सीमित है और वैश्विक स्तर तक पहुंचने वाले स्व-नियमन के एक झरने के रूप में, ग्रह के सभी पारिस्थितिक तंत्रों और जैव प्रणालियों में होती है। वैश्विक आवास के स्वचालित रखरखाव का नियम वी.आई. के जैव-भू-रासायनिक सिद्धांतों का पालन करता है। वर्नाडस्की, प्रजातियों के आवासों के संरक्षण के नियम, सापेक्ष आंतरिक स्थिरता और जीवमंडल में रूढ़िवादी तंत्र की उपस्थिति के लिए एक स्थिरांक के रूप में कार्य करता है और साथ ही सिस्टम-गतिशील संपूरकता के नियम की पुष्टि करता है। जीवमंडल पर ब्रह्मांडीय प्रभाव ब्रह्मांडीय प्रभावों के अपवर्तन के नियम से प्रमाणित होता है: जीवमंडल और विशेष रूप से इसके उपखंडों पर प्रभाव डालने वाले ब्रह्मांडीय कारक, ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा परिवर्तन के अधीन हैं और इसलिए, ताकत और समय के संदर्भ में , अभिव्यक्तियाँ कमजोर हो सकती हैं और स्थानांतरित हो सकती हैं या पूरी तरह से अपना प्रभाव खो सकती हैं। यहां सामान्यीकरण इस तथ्य के कारण महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र और इसमें रहने वाले जीवों पर अक्सर सौर गतिविधि और अन्य ब्रह्मांडीय कारकों के समकालिक प्रभावों का प्रवाह होता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पृथ्वी और उसके जीवमंडल में कई प्रक्रियाएं, हालांकि अंतरिक्ष के प्रभाव के अधीन हैं, सौर गतिविधि के चक्र 1850, 600, 400, 178, 169, 88, 83, 33, 22, 16 के अंतराल के साथ माने जाते हैं। , 11, 5 (11 ,1), 6.5 और 4.3 वर्ष, जीवमंडल और उसके प्रभागों को सभी मामलों में समान चक्रीयता के साथ प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। जीवमंडल प्रणाली के ब्रह्मांडीय प्रभावों को पूरी तरह या आंशिक रूप से अवरुद्ध किया जा सकता है। निष्कर्ष पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी में बुनियादी कार्यात्मक इकाई हैं, क्योंकि इनमें जीव और निर्जीव पर्यावरण शामिल हैं - ऐसे घटक जो एक-दूसरे के गुणों और पृथ्वी पर मौजूद जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को परस्पर प्रभावित करते हैं। जीवित जीवों के समुदाय (बायोसेनोसिस) के साथ एक विशिष्ट भौतिक रासायनिक वातावरण (बायोटोप) का संयोजन एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। माइक्रोइकोसिस्टम, मेसोइकोसिस्टम और वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र - जीवमंडल हैं। पारिस्थितिक तंत्र अव्यवस्था में बिखरे हुए नहीं हैं; इसके विपरीत, वे क्षैतिज (अक्षांश में) और लंबवत (ऊंचाई में) दोनों, काफी नियमित क्षेत्रों में समूहीकृत हैं। पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाला सौर विकिरण 1.54 मिलियन EJ प्रति वर्ष है। ग्रह की सतह तक पहुंचने वाली अधिकांश सौर ऊर्जा सीधे गर्मी, पानी या मिट्टी को गर्म करने में परिवर्तित हो जाती है, जो बदले में हवा को गर्म करती है। पारिस्थितिकी तंत्र गैर-प्रदूषणकारी और लगभग शाश्वत सौर ऊर्जा के कारण अस्तित्व में है, जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत स्थिर और प्रचुर है। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा पदार्थों के दो चक्रों का कारण बनती है: बड़े, या भूवैज्ञानिक, और छोटे, जैविक (जैविक)। दोनों चक्र परस्पर जुड़े हुए हैं और मानो एक ही प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैव-भू-रासायनिक चक्र, या जैव-भू-रासायनिक चक्रों का अस्तित्व, प्रणाली के स्व-नियमन (होमियोस्टैसिस) के लिए अवसर पैदा करता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिरता देता है: विभिन्न तत्वों की प्रतिशत सामग्री की एक अद्भुत स्थिरता। पदार्थों के बहुत सारे चक्र होते हैं। स्थानांतरित द्रव्यमान और ऊर्जा खपत के संदर्भ में पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण चक्र ग्रहीय जल विज्ञान चक्र या जल चक्र है। जैविक (जैविक) चक्र मिट्टी, पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों के बीच पदार्थों के परिसंचरण को संदर्भित करता है। सभी जैव-भू-रासायनिक चक्रों में से, कार्बन चक्र निस्संदेह सबसे तीव्र है। भूवैज्ञानिक युगों के दौरान उत्पादित अधिकांश ऑक्सीजन वायुमंडल में नहीं रहती थी, बल्कि कार्बोनेट, सल्फेट्स, आयरन ऑक्साइड आदि के रूप में स्थलमंडल द्वारा स्थिर होती थी। यह द्रव्यमान 590x1014 टन बनाम 39x1014 टन ऑक्सीजन है, जो जीवमंडल में प्रसारित होता है। महाद्वीपीय और समुद्री जल में घुली गैस या सल्फेट के रूप में। नाइट्रोजन एक आवश्यक बायोजेनिक तत्व है, क्योंकि यह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा है। नाइट्रोजन चक्र सबसे जटिल में से एक है, क्योंकि इसमें गैस और खनिज दोनों चरण शामिल हैं, और साथ ही सबसे आदर्श चक्र भी शामिल हैं। जीवमंडल में फास्फोरस चक्र पौधों और जानवरों में चयापचय प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। प्रोटोप्लाज्म का यह महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व, स्थलीय पौधों और शैवाल में 0.01-0.1%, जानवरों में 0.1% से कई प्रतिशत तक निहित होता है, घूमता है, धीरे-धीरे कार्बनिक यौगिकों से फॉस्फेट में बदल जाता है, जिसे फिर से पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। कई गैसीय सल्फर यौगिक हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। जीवों की महत्वपूर्ण गतिविधि को बनाए रखना और पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थ के संचलन को बनाए रखना, यानी पारिस्थितिक तंत्र का अस्तित्व, सभी जीवों के लिए उनके महत्वपूर्ण कार्यों और आत्म-प्रजनन के लिए आवश्यक ऊर्जा के निरंतर प्रवाह पर निर्भर करता है। उन पदार्थों के विपरीत जो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न ब्लॉकों के माध्यम से लगातार घूमते रहते हैं, जिन्हें हमेशा पुन: उपयोग किया जा सकता है और चक्र में प्रवेश किया जा सकता है, ऊर्जा का उपयोग एक बार किया जा सकता है, यानी, पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा का एक रैखिक प्रवाह होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर, ऊर्जा युक्त पदार्थ स्वपोषी जीवों द्वारा बनाए जाते हैं और विषमपोषी जीवों के लिए भोजन के रूप में काम करते हैं। खाद्य कनेक्शन एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा स्थानांतरित करने के तंत्र हैं। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर, खाद्य जालों की एक अच्छी तरह से परिभाषित संरचना होती है, जो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के प्रत्येक स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले जीवों की प्रकृति और संख्या की विशेषता होती है। पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण एक गतिशील प्रक्रिया है। पारिस्थितिक तंत्र में, उनके सदस्यों की स्थिति और महत्वपूर्ण गतिविधि और आबादी के अनुपात में परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। किसी भी समुदाय में होने वाले विविध परिवर्तन दो मुख्य प्रकारों में आते हैं: चक्रीय और प्रगतिशील। उत्तराधिकार एक प्राकृतिक, निर्देशित प्रक्रिया है और एक या दूसरे चरण में होने वाले परिवर्तन किसी भी समुदाय की विशेषता होते हैं और इसकी प्रजाति संरचना या भौगोलिक स्थिति पर निर्भर नहीं होते हैं। वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जीवमंडल को जियोबायोस्फीयर, हाइड्रोबायोस्फीयर और एरोबायोस्फीयर में विभाजित किया गया है। जीवमंडल का निर्माण काफी हद तक बाहरी कारकों से नहीं, बल्कि आंतरिक पैटर्न से होता है। जीवमंडल की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति जीवित और निर्जीव चीजों की परस्पर क्रिया है, जो वी.आई. द्वारा परमाणुओं के बायोजेनिक प्रवासन के नियम में परिलक्षित होती है। वर्नाडस्की। पृथ्वी पर मौजूद पारिस्थितिक तंत्र विविध हैं। इसमें माइक्रोइकोसिस्टम (उदाहरण के लिए, एक सड़ते हुए पेड़ का तना), मेसोइकोसिस्टम (जंगल, तालाब, आदि), मैक्रोइकोसिस्टम (महाद्वीप, महासागर, आदि) और वैश्विक जीवमंडल हैं। बड़े स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बायोम कहा जाता है। प्रत्येक बायोम में कई छोटे, परस्पर जुड़े हुए पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के कई वर्गीकरण हैं: सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन; रेगिस्तान: घासयुक्त और झाड़ीदार; उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और सवाना; समशीतोष्ण मैदान; शीतोष्ण पर्णपाती वन: बोरियल शंकुधारी वन। टुंड्रा: आर्कटिक और अल्पाइन। मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार: रिबन (स्थिर पानी): झीलें, तालाब, आदि; लोटिक (बहता पानी): नदियाँ, झरने, आदि; आर्द्रभूमियाँ: दलदल और दलदली जंगल; समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार: खुला महासागर (पेलजिक); महाद्वीपीय शेल्फ का जल (तटीय जल); उत्थान क्षेत्र (उत्पादक मत्स्य पालन के साथ उपजाऊ क्षेत्र); मुहाना (तटीय खाड़ियाँ, जलडमरूमध्य, नदी के मुहाने, नमक दलदल, आदि)। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक होते हैं: जीव और उनके निर्जीव पर्यावरण के कारक। जीवों (पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव) की समग्रता को पारिस्थितिकी तंत्र का बायोटा कहा जाता है। विभिन्न श्रेणियों के जीवों के बीच परस्पर क्रिया के तरीके ही उसकी जैविक संरचना हैं। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा पदार्थों के दो चक्रों का कारण बनती है: एक बड़ा, या भूवैज्ञानिक, जल चक्र और वायुमंडलीय परिसंचरण में सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, और एक छोटा, जैविक (बायोटिक), एक बड़े के आधार पर विकसित होता है और निरंतर होता है, चक्रीय, लेकिन समय और स्थान में असमान, और संगठन के विभिन्न स्तरों के पारिस्थितिक प्रणालियों के भीतर पदार्थ, ऊर्जा और सूचना के प्राकृतिक पुनर्वितरण में कम या ज्यादा महत्वपूर्ण नुकसान के साथ। दोनों चक्र परस्पर जुड़े हुए हैं और मानो एक ही प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक कारकों और जीवित जीवों की परस्पर क्रिया के साथ वैकल्पिक कार्बनिक और खनिज यौगिकों के रूप में बायोटोप और बायोकेनोसिस के बीच पदार्थ का निरंतर संचलन होता है। जीवित जीवों और अकार्बनिक पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों का आदान-प्रदान, जिसके विभिन्न चरण एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर होते हैं, को जैव-भू-रासायनिक चक्र या जैव-भू-रासायनिक चक्र कहा जाता है। ऐसे चक्रों का अस्तित्व सिस्टम के स्व-नियमन (होमियोस्टैसिस) के लिए अवसर पैदा करता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिरता देता है: विभिन्न तत्वों के प्रतिशत की एक अद्भुत स्थिरता। पारिस्थितिक तंत्र के कामकाज का सिद्धांत यहां लागू होता है: संसाधनों का अधिग्रहण और कचरे का निपटान सभी तत्वों के चक्र के ढांचे के भीतर होता है। प्रयुक्त साहित्य की सूची 1.बिगॉन एम.आई. पारिस्थितिकी, व्यक्ति, आबादी और समुदाय। एम.: 1989. - 290 पी। 2.बेयसेनोवा ए.एस., शिल्डेबाएव जे.एच.बी., सौतबाएवा जी.जेड. पारिस्थितिकी। अल्माटी: "जिल्म, 2001. - 201 पी। 3.अकीमोवा टी.ए., खस्किन वी.वी. पारिस्थितिकी। एम.: यूनिटी पब्लिशिंग हाउस, 1998. - 233 पी। .गोरेलोव ए.ए. पारिस्थितिकी। व्याख्यान पाठ्यक्रम. एम.: "सेंटर" 1997. - 280 पी। .स्टैडनिट्स्की जी.वी., रोडियोनोव ए.आई. पारिस्थितिकी। एम.: यूनिटी पब्लिशिंग हाउस, 1996. - 272 पी। .सदानोव ए.के., स्वानबायेवा जेड.एस., पारिस्थितिकी। अल्माटी: "एग्रोयूनिवर्सिटी", 1999. - 197 पी। .शिलोव आई.ए. पारिस्थितिकी। एम.: हायर स्कूल, 2000. - 348 पी। .रीमर्स एन.एफ. पारिस्थितिकी (सिद्धांत, कानून, नियम, सिद्धांत और परिकल्पना)। एम.: "यंग रशिया", 1994. - 260 पी। .स्वेत्कोवा एल.आई., अलेक्सेव एम.आई., उसेनोव बी.पी. और अन्य। पारिस्थितिकी। तकनीकी विश्वविद्यालयों के लिए पाठ्यपुस्तक। एम।; एएसवी, सेंट पीटर्सबर्ग: खिमिज़दत, 1999, 185 पी। .गिरुसोव ई.वी. पर्यावरण प्रबंधन की पारिस्थितिकी और अर्थशास्त्र। एम.: कानून और कानून, एकता। 1998 - 232 पी. .व्रोन्स्की वी.ए. अनुप्रयुक्त पारिस्थितिकी: पाठ्यपुस्तक। फ़ायदा। रोस्तोव-ऑन-डॉन: 1995. - 197 पी। .बुड्यको एम.आई. वैश्विक पारिस्थितिकी. एम.: माइसल, 1977.-248 पी। .अलेक्सेन्को वी.ए. पर्यावरण भू-रसायन विज्ञान. पाठ्यपुस्तक। एम.: लोगो, 2000 - 410 पी। .पेत्रोव के.एम. एस-पी की सामान्य पारिस्थितिकी। ट्यूटोरियल। "रसायन विज्ञान", 1997. - 218 पी। .एंडरसन जे.एम. पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान. जीवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, मनुष्य। एल., 1985. 376 पी. .गिरेनोक एफ.आई. पारिस्थितिकी। सभ्यता। नोस्फीयर.एम.: 191987. - 281 पी. .संतुलन की तलाश में: सामाजिक-राजनीतिक प्राथमिकताओं की प्रणाली में पारिस्थितिकी एम.: 1992. - 427 पी। .समाज और प्रकृति के बीच अंतःक्रिया का इतिहास: कारक और अवधारणा। एम.: एएनएसएसएसआर 1990। .स्टेपानोव्स्की ए.एस. अनुप्रयुक्त पारिस्थितिकी: पर्यावरण संरक्षण। विश्वविद्यालयों के लिए पाठ्यपुस्तक. एम.: एकता दाना. 2003. 751 पी. समान कार्य - पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों और ऊर्जा प्रवाह का चक्र
"पदार्थ का प्रवाह" और "ऊर्जा का प्रवाह" शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। पदार्थ का प्रवाह रासायनिक तत्वों और उनके यौगिकों के रूप में उत्पादकों से डीकंपोजर (उपभोक्ताओं के माध्यम से या उनके बिना) तक की गति है। ऊर्जा प्रवाह एक पोषी स्तर से दूसरे (उच्च) तक खाद्य श्रृंखलाओं के साथ कार्बनिक यौगिकों (भोजन) के रासायनिक बंधों के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, उन पदार्थों के विपरीत जो लगातार पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न ब्लॉकों के माध्यम से घूमते हैं और हमेशा चक्र में फिर से प्रवेश कर सकते हैं, आने वाली ऊर्जा का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है।
एक सार्वभौमिक प्राकृतिक घटना के रूप में, ऊर्जा का एकतरफा प्रवाह थर्मोडायनामिक्स के नियमों द्वारा निर्धारित होता है। पहले नियम के अनुसार, ऊर्जा एक रूप (प्रकाश की ऊर्जा) से दूसरे (भोजन की संभावित ऊर्जा) में जा सकती है, लेकिन यह दोबारा कभी नहीं बनती है और बिना किसी निशान के गायब नहीं होती है।
थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहता है कि ऊर्जा के परिवर्तन से जुड़ी एक भी प्रक्रिया इसका कुछ हिस्सा खोए बिना नहीं हो सकती है। इस कारण से, 100% दक्षता के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, उदाहरण के लिए, भोजन का उस पदार्थ में जिससे जीव का शरीर बना है।
इस प्रकार, सभी पारिस्थितिक तंत्रों की कार्यप्रणाली ऊर्जा के निरंतर प्रवाह से निर्धारित होती है, जो सभी जीवों के अस्तित्व और आत्म-प्रजनन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
पारिस्थितिक तंत्र में प्रतिस्पर्धी संबंध भी होते हैं। इस पहलू में, ऊर्जा अधिकतमकरण का नियम (जी. ओडुम - ई. ओडुम) बहुत रुचिकर है: अन्य पारिस्थितिक तंत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा में, जो ऊर्जा की आपूर्ति में सबसे अच्छा योगदान देता है और इसकी अधिकतम मात्रा का सबसे कुशल तरीके से उपयोग करता है वह जीवित रहता है। (संरक्षित करता है)। कानून के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए प्रणाली: 1) उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा (उदाहरण के लिए, वसा भंडार) के संचयक (भंडार) बनाती है; 2) नई ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संचित ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा खर्च करता है; 3) विभिन्न पदार्थों का संचलन सुनिश्चित करता है; 4) नियामक तंत्र बनाता है जो सिस्टम की स्थिरता और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता का समर्थन करता है; 5) विशेष प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य प्रणालियों के साथ आदान-प्रदान स्थापित करता है।
एक महत्वपूर्ण परिस्थिति पर जोर देना आवश्यक है: ऊर्जा अधिकतमीकरण का नियम सूचना के संबंध में भी मान्य है, इसलिए (एन.एफ. रीमर्स के अनुसार) इसे ऊर्जा और सूचना अधिकतमीकरण का नियम भी माना जा सकता है: वह प्रणाली जो सबसे अधिक योगदान देती है ऊर्जा और सूचना की प्राप्ति, उत्पादन और प्रभावी उपयोग।
आइए ध्यान दें कि किसी पदार्थ की अधिकतम आपूर्ति, अन्य समान प्रणालियों के प्रतिस्पर्धी समूह में सिस्टम की सफलता की गारंटी नहीं देती है।
पहले यह नोट किया गया था कि बायोकेनोसिस के जीवों के बीच मजबूत खाद्य संबंध या खाद्य श्रृंखला उत्पन्न होती है और स्थापित होती है। उत्तरार्द्ध में तीन मुख्य लिंक होते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और डीकंपोजर।
प्रकाश संश्लेषक जीवों से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखलाओं को चराई (या चराई) श्रृंखला कहा जाता है, और जो श्रृंखलाएं मृत पौधों के पदार्थ, शवों और जानवरों के मलमूत्र से शुरू होती हैं उन्हें डेट्राइटल श्रृंखला कहा जाता है।
खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक कड़ी के स्थान को पोषी स्तर कहा जाता है; यह पदार्थों और ऊर्जा के प्रवाह की विभिन्न तीव्रताओं की विशेषता है। प्रथम पोषी स्तर हमेशा उत्पादक होता है; दूसरा - शाकाहारी उपभोक्ता; तीसरा - मांसाहारी, शाकाहारी रूपों में रहने वाले; चौथा स्तर - अन्य मांसाहारियों का सेवन करना आदि।
खाद्य श्रृंखला में विभिन्न स्तरों पर रहने वाले पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्रम के उपभोक्ता हैं (चित्र 9)।
चावल। 9.
जाहिर है कि उपभोक्ताओं की खाद्य विशेषज्ञता इसमें प्रमुख भूमिका निभाती है। पोषण की एक विस्तृत श्रृंखला वाली प्रजातियों को विभिन्न पोषी स्तरों पर खाद्य श्रृंखलाओं में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के आहार में पौधों के खाद्य पदार्थ और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का मांस शामिल होता है। इसलिए, यह विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं में I, II या III ऑर्डर के उपभोक्ता के रूप में कार्य करता है।
चूंकि ऊर्जा को एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित करते समय ऊर्जा खो जाती है, इसलिए बिजली श्रृंखला लंबी नहीं हो सकती: इसमें आमतौर पर 4...6 लिंक होते हैं (तालिका 1)।
1. खाद्य श्रृंखलाओं के विशिष्ट चित्र (वी. एम. इवोनिन के अनुसार, 1996)
हालाँकि, अपने शुद्ध रूप में ऐसी श्रृंखलाएँ आमतौर पर प्रकृति में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि एक ही प्रजाति अलग-अलग कड़ियों में एक साथ मौजूद हो सकती है। यह इस तथ्य के कारण है कि प्रकृति में कुछ मोनोफेज हैं; ऑलिगोफेज और पॉलीफेज बहुत अधिक सामान्य हैं। उदाहरण के लिए, विभिन्न शाकाहारी और मांसाहारी जीवों को खाने वाले शिकारी कई श्रृंखलाओं की कड़ियाँ हैं। परिणामस्वरूप, प्रत्येक बायोसेनोसिस में खाद्य श्रृंखलाओं के परिसरों का विकास क्रमिक रूप से होता है, जो एक संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार बिजली नेटवर्क बनाए जाते हैं, जो बहुत जटिल होते हैं।
इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला समुदाय में ऊर्जा हस्तांतरण का मुख्य चैनल है (पौधों - उत्पादकों, जानवरों - उपभोक्ताओं और सूक्ष्मजीवों - डीकंपोजर के बीच) (चित्र 10)। आरेख में पहले से ही यह स्पष्ट है कि का विचार खाद्य श्रृंखलाएं और पोषी स्तर एक अमूर्त बात है। स्पष्ट रूप से अलग-अलग स्तरों के साथ एक रैखिक श्रृंखला प्रयोगशाला में बनाई जा सकती है। लेकिन प्रकृति में वास्तव में पोषी नेटवर्क होते हैं जिनमें कई आबादी एक साथ कई पोषी स्तरों से संबंधित होती हैं। एक ही जीव उपभोग करता है जानवर और पौधे दोनों; शिकारी पहले और दूसरे क्रम के उपभोक्ताओं को खा सकते हैं; कई जानवर जीवित और मृत दोनों पौधों को खाते हैं।
पोषी संबंधों की जटिलता के कारण, एक प्रजाति के नष्ट होने से अक्सर समुदाय पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अन्य "उपयोगकर्ता" विलुप्त प्रजातियों का भोजन खाना शुरू कर देते हैं,

चावल। 10.
जो प्रजातियाँ इस पर भोजन करती हैं वे भोजन के नए स्रोत ढूंढती हैं: सामान्य तौर पर, समुदाय में संतुलन बना रहता है।
उत्पादकों द्वारा अवशोषित ऊर्जा खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से प्रवाहित होती है और धीरे-धीरे उपभोग की जाती है। खाद्य श्रृंखला के अंत में ऊर्जा की मात्रा हमेशा शुरुआत की तुलना में कम होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान, पौधे उन पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का औसतन केवल 1% ही बांध पाते हैं। एक जानवर जिसने एक पौधा खाया है वह भोजन का कुछ हिस्सा पचा नहीं पाता है और उसे मल के रूप में बाहर निकाल देता है। आमतौर पर पौधों का 20...60% भोजन पच जाता है; अवशोषित ऊर्जा का उपयोग पशु के जीवन को बनाए रखने के लिए किया जाता है। कोशिकाओं और अंगों का कामकाज गर्मी की रिहाई के साथ होता है, यानी, जिससे खाद्य ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जल्द ही पर्यावरण में नष्ट हो जाता है। भोजन का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा नए ऊतकों के निर्माण और वसा भंडार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद, एक शिकारी जिसने एक शाकाहारी जानवर को खा लिया है और तीसरे ट्रॉफिक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, उसे पौधे द्वारा संचित ऊर्जा से केवल वह ऊर्जा प्राप्त होती है जो बायोमास में वृद्धि के रूप में उसके शिकार (दूसरे स्तर) के शरीर में बरकरार रहती है।
यह ज्ञात है कि खाद्य श्रृंखला में पदार्थ और ऊर्जा के स्थानांतरण के दौरान प्रत्येक चरण में, लगभग 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है और इसका केवल दसवां हिस्सा ही अगले उपभोक्ता तक पहुंचता है, यानी, खाद्य कनेक्शन में ऊर्जा का स्थानांतरण जीवों की संख्या "दस प्रतिशत नियम" (लिंडमैन का सिद्धांत) का पालन करती है। उदाहरण के लिए, तृतीयक मांसाहारी (पांचवें पोषी स्तर) तक पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा उत्पादकों द्वारा अवशोषित ऊर्जा का केवल 10 -4 है। यह बायोकेनोसिस की प्रजातियों की संरचना की जटिलता की परवाह किए बिना, खाद्य श्रृंखला में लिंक (स्तरों) की सीमित संख्या (5...6) की व्याख्या करता है।

चावल। ग्यारह।
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए, यह समझना भी आसान है कि पोषी स्तर बढ़ने पर बायोमास क्यों कम हो जाता है। यहां पारिस्थितिक तंत्र के कामकाज का तीसरा बुनियादी सिद्धांत प्रकट होता है: किसी आबादी का बायोमास जितना अधिक होगा, उसका पोषी स्तर उतना ही कम होना चाहिए, अन्यथा: लंबी खाद्य श्रृंखलाओं के अंत में एक बड़ा बायोमास नहीं हो सकता है।
ऊपर सूचीबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज के तीन बुनियादी सिद्धांत - पोषक तत्वों का चक्र, सौर ऊर्जा का प्रवाह और बढ़ते पोषी स्तर के साथ बायोमास में कमी - को एक सामान्य आरेख (छवि 11) के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि हम जीवों को उनके पोषण संबंधों के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, उनमें से प्रत्येक के लिए ऊर्जा और पोषक तत्वों के "इनपुट" और "आउटपुट" का संकेत देते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पोषक तत्वों को पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर लगातार पुनर्चक्रित किया जाता है, और ऊर्जा का प्रवाह इसके माध्यम से गुजरता है।
जीवों की महत्वपूर्ण गतिविधि को बनाए रखना और पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थ के संचलन को बनाए रखना, यानी पारिस्थितिक तंत्र का अस्तित्व, सभी जीवों के लिए उनके महत्वपूर्ण कार्यों और आत्म-प्रजनन के लिए आवश्यक ऊर्जा के निरंतर प्रवाह पर निर्भर करता है।
उन पदार्थों के विपरीत जो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न ब्लॉकों के माध्यम से लगातार घूमते रहते हैं, जिन्हें हमेशा पुन: उपयोग किया जा सकता है और चक्र में प्रवेश किया जा सकता है, ऊर्जा का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है, यानी, पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा का एक रैखिक प्रवाह होता है।
एक सार्वभौमिक प्राकृतिक घटना के रूप में ऊर्जा का एकतरफा प्रवाह थर्मोडायनामिक्स के नियमों के परिणामस्वरूप होता है। पहला कानूनबताता है कि ऊर्जा को एक रूप (जैसे प्रकाश) से दूसरे रूप (जैसे भोजन की संभावित ऊर्जा) में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरा कानूनकहा गया है कि ऊर्जा के परिवर्तन से जुड़ी एक भी प्रक्रिया इसका कुछ हिस्सा खोए बिना नहीं हो सकती है। ऐसे परिवर्तनों में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा दुर्गम तापीय ऊर्जा में नष्ट हो जाती है और इसलिए नष्ट हो जाती है। इसलिए, उदाहरण के लिए, खाद्य पदार्थों का जीव के शरीर को बनाने वाले पदार्थ में परिवर्तन नहीं हो सकता है, जो 100 प्रतिशत दक्षता के साथ होता है।
इस प्रकार, जीवित जीव ऊर्जा परिवर्तक हैं। और हर बार जब ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो इसका कुछ हिस्सा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाता है। अंततः, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक चक्र में प्रवेश करने वाली सारी ऊर्जा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है। जीवित जीव वास्तव में काम करने के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में गर्मी का उपयोग नहीं करते हैं - वे प्रकाश और रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं।
पारिस्थितिक पिरामिड.प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर, खाद्य जालों की एक अच्छी तरह से परिभाषित संरचना होती है, जो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के प्रत्येक स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले जीवों की प्रकृति और संख्या की विशेषता होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन करने और उन्हें ग्राफिक रूप से चित्रित करने के लिए, वे आमतौर पर खाद्य वेब आरेखों के बजाय पारिस्थितिक पिरामिड का उपयोग करते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र की पोषी संरचना को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं। इनका निर्माण समान चौड़ाई के आयतों के रूप में किया जाता है, लेकिन आयतों की लंबाई मापी जाने वाली वस्तु के मान के समानुपाती होनी चाहिए। यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं संख्या, बायोमास और ऊर्जा के पिरामिड।
पारिस्थितिक पिरामिड किसी भी बायोकेनोसिस की मूलभूत विशेषताओं को दर्शाते हैं जब वे इसकी ट्रॉफिक संरचना दिखाते हैं:
उनकी ऊंचाई प्रश्न में खाद्य श्रृंखला की लंबाई के समानुपाती होती है, यानी, इसमें मौजूद पोषी स्तरों की संख्या;
उनका आकार कमोबेश एक स्तर से दूसरे स्तर पर संक्रमण के दौरान ऊर्जा परिवर्तन की दक्षता को दर्शाता है।
संख्याओं के पिरामिड.वे किसी पारिस्थितिकी तंत्र की पोषी संरचना के अध्ययन के लिए सबसे सरल सन्निकटन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मामले में, किसी दिए गए क्षेत्र में जीवों की संख्या को पहले गिना जाता है, ट्रॉफिक स्तरों के आधार पर समूहीकृत किया जाता है और एक आयत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी लंबाई (या क्षेत्र) किसी दिए गए क्षेत्र में रहने वाले जीवों की संख्या के समानुपाती होती है ( या किसी दिए गए आयतन में, यदि यह एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है)। एक बुनियादी नियम स्थापित किया गया है कि किसी भी वातावरण में जानवरों की तुलना में अधिक पौधे, मांसाहारी की तुलना में अधिक शाकाहारी, पक्षियों की तुलना में अधिक कीड़े आदि होते हैं।
जनसंख्या पिरामिड प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों के घनत्व को दर्शाते हैं। विभिन्न जनसंख्या पिरामिडों के निर्माण में बहुत विविधता है। अक्सर ये उल्टे होते हैं.
उदाहरण के लिए, एक जंगल में कीड़े (शाकाहारी) की तुलना में काफी कम पेड़ (प्राथमिक उत्पादक) होते हैं।
बायोमास पिरामिड.पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य संबंधों को अधिक पूर्ण रूप से दर्शाता है, क्योंकि यह जीवों के कुल द्रव्यमान को ध्यान में रखता है (बायोमास)प्रत्येक पोषी स्तर. बायोमास पिरामिड में आयतें प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर प्रति इकाई क्षेत्र या आयतन पर जीवों के द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करती हैं। बायोमास पिरामिड का आकार अक्सर जनसंख्या पिरामिड के आकार के समान होता है। प्रत्येक क्रमिक पोषी स्तर पर बायोमास में कमी विशेषता है।
बायोमास के पिरामिड, साथ ही संख्याएँ, न केवल सीधे, बल्कि उल्टे भी हो सकते हैं। बायोमास के उल्टे पिरामिड जलीय पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता हैं, जिसमें प्राथमिक उत्पादक, जैसे फाइटोप्लांकटोनिक शैवाल, बहुत तेज़ी से विभाजित होते हैं, और उनके उपभोक्ता - ज़ोप्लांकटोनिक क्रस्टेशियंस - बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनका प्रजनन चक्र लंबा होता है। विशेष रूप से, यह मीठे पानी के वातावरण पर लागू होता है, जहां प्राथमिक उत्पादकता सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदान की जाती है जिनकी चयापचय दर बढ़ जाती है, यानी, बायोमास कम है, उत्पादकता अधिक है।
ऊर्जा का पिरामिड.विभिन्न पोषी स्तरों पर जीवों के बीच संबंध प्रदर्शित करने का सबसे मौलिक तरीका ऊर्जा पिरामिड के माध्यम से है। वे खाद्य श्रृंखलाओं की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता और उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रति इकाई सतह क्षेत्र में प्रति इकाई समय में संचित ऊर्जा (केकेसी) की मात्रा की गणना करके और प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों द्वारा उपयोग की जाती है। इस प्रकार, बायोमास में संग्रहीत ऊर्जा की मात्रा निर्धारित करना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन प्रत्येक पोषी स्तर पर अवशोषित ऊर्जा की कुल मात्रा का अनुमान लगाना अधिक कठिन है। एक ग्राफ़ (चित्र 12.28) बनाने के बाद, हम बता सकते हैं कि विध्वंसक, जिनका महत्व बायोमास पिरामिड में छोटा लगता है, और जनसंख्या पिरामिड में इसके विपरीत; पारिस्थितिकी तंत्र से गुजरने वाली ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त करें। इसके अलावा, इस सारी ऊर्जा का केवल एक हिस्सा पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर जीवों में रहता है और बायोमास में संग्रहीत होता है; बाकी का उपयोग जीवित प्राणियों की चयापचय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है: अस्तित्व, विकास, प्रजनन को बनाए रखना। पशु मांसपेशियों के काम के लिए भी काफी मात्रा में ऊर्जा खर्च करते हैं।
आर. लिंडमैन ने पहली बार 1942 में तैयार किया ऊर्जा पिरामिड नियम,जिसे पाठ्यपुस्तकों में अक्सर "10% का नियम" कहा जाता है। इस कानून के अनुसार, एक से पारिस्थितिक पिरामिड का पोषी स्तरऔसतन, 10% से अधिक ऊर्जा दूसरे स्तर पर नहीं जाती है।
उपभोक्ता पारिस्थितिकी तंत्र में प्रबंधन और स्थिरीकरण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। उपभोक्ता प्रभुत्वशाली लोगों के एकाधिकार को रोकते हुए, सेनोसिस में विविधता का एक स्पेक्ट्रम उत्पन्न करते हैं। उपभोक्ताओं के मूल्य नियंत्रण का नियमउचित रूप से काफी मौलिक माना जा सकता है। साइबरनेटिक विचारों के अनुसार, नियंत्रण प्रणाली की संरचना नियंत्रित प्रणाली से अधिक जटिल होनी चाहिए, तब उपभोक्ता प्रकारों की बहुलता का कारण स्पष्ट हो जाता है। उपभोक्ताओं के नियंत्रण महत्व का भी एक ऊर्जावान आधार है। एक या दूसरे पोषी स्तर के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह अंतर्निहित पोषी स्तर में भोजन की उपलब्धता से पूरी तरह से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि ज्ञात है, हमेशा पर्याप्त "भंडार" बचा रहता है, क्योंकि भोजन के पूर्ण विनाश से उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाएगी। ये सामान्य पैटर्न जनसंख्या प्रक्रियाओं, समुदायों, पारिस्थितिक पिरामिड के स्तर और समग्र रूप से बायोकेनोज के ढांचे के भीतर देखे जाते हैं।
प्रस्तुति पूर्वावलोकन का उपयोग करने के लिए, एक Google खाता बनाएं और उसमें लॉग इन करें: https://accounts.google.com
स्लाइड कैप्शन:
प्रकृति में पदार्थ और ऊर्जा का चक्र
पदार्थों का चक्र प्रकृति में पदार्थ के परिवर्तन और गति की दोहराई जाने वाली प्रक्रियाएं हैं, जो कमोबेश चक्रीय होती हैं। हमारे ग्रह पर सभी पदार्थ परिसंचरण की प्रक्रिया में हैं। प्रकृति में दो मुख्य चक्र हैं: बड़ा (भूवैज्ञानिक) छोटा (जैव भू-रासायनिक)
पदार्थों का महान चक्र महान चक्र लाखों वर्षों तक चलता है और यह पृथ्वी की गहरी ऊर्जा के साथ सौर ऊर्जा की परस्पर क्रिया के कारण होता है। भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, चट्टानों के निर्माण और विनाश और विनाश उत्पादों के बाद के आंदोलन से जुड़ा हुआ है।
पदार्थों का छोटा चक्र छोटा चक्र (बायोजियोकेमिकल) जीवमंडल के भीतर, बायोकेनोसिस के स्तर पर होता है। इसका सार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान अकार्बनिक यौगिकों से जीवित पदार्थ का निर्माण और अपघटन के दौरान कार्बनिक पदार्थों का वापस अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन है। जैव-भू-रासायनिक चक्र - वर्नाडस्की वी.आई.
जल चक्र Tr अपवाह inf जल वाष्पीकरण वाष्प संघनन वर्षा अपवाह वाष्पोत्सर्जन अंतःस्यंदन
वाष्पोत्सर्जन एक पौधे के माध्यम से पानी के प्रवाहित होने और पौधे के बाहरी अंगों, जैसे पत्तियों, तनों और फूलों के माध्यम से इसके वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। पानी पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जड़ों के माध्यम से आपूर्ति किए गए पानी का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही सीधे विकास और चयापचय के लिए उपयोग किया जाता है।
जल चक्र
जल चक्र अधिकांश पानी महासागरों में केंद्रित है। उनकी सतह से वाष्पित होने वाला पानी प्राकृतिक और कृत्रिम भूमि पारिस्थितिकी तंत्र की आपूर्ति करता है। कोई क्षेत्र समुद्र के जितना करीब होगा, वहां उतनी ही अधिक वर्षा होगी। भूमि लगातार समुद्र में पानी लौटाती है: कुछ नमी वाष्पित हो जाती है, सबसे सक्रिय रूप से जंगलों में, कुछ नदियों द्वारा एकत्र किया जाता है: वे बारिश प्राप्त करते हैं और पानी पिघलाते हैं। समुद्र और ज़मीन के बीच नमी के आदान-प्रदान के लिए बहुत अधिक ऊर्जा लागत की आवश्यकता होती है: पृथ्वी तक पहुँचने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 30% इसी पर खर्च होता है।
जल चक्र पर मानव का प्रभाव सभ्यता के विकास से पहले जीवमंडल में जल चक्र संतुलन में था, अर्थात। समुद्र को नदियों से उतना ही पानी प्राप्त होता था जितना वह वाष्पीकरण के माध्यम से उपयोग करता था। सभ्यता के विकास के साथ-साथ यह चक्र बाधित होने लगा। विशेष रूप से, जंगल कम से कम पानी का वाष्पीकरण करते हैं क्योंकि... उनका क्षेत्र घट रहा है, और मिट्टी की सतह, इसके विपरीत, बढ़ रही है, क्योंकि सिंचित कृषि भूमि का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। भूमि. दक्षिणी क्षेत्रों की नदियाँ उथली हो गईं। समुद्र की सतह से पानी अधिक तेजी से वाष्पित होता है, क्योंकि... इसका एक महत्वपूर्ण भाग तेल की परत से ढका हुआ है। यह सब जीवमंडल में जल आपूर्ति को खराब करता है।
सूखा लगातार बढ़ता जा रहा है, और पर्यावरणीय आपदाएँ उभर रही हैं। उदाहरण के लिए, अफ्रीका में साहेल क्षेत्र में, जो एक अर्ध-रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो सहारा को महाद्वीप के उत्तरी देशों से अलग करता है, 35 वर्षों से अधिक समय तक विनाशकारी सूखा पड़ा है। ताज़ा पानी जो ज़मीन से समुद्र और अन्य जल निकायों में लौटता है, अक्सर प्रदूषित होता है। कई रूसी नदियों का पानी पीने के लिए व्यावहारिक रूप से अनुपयुक्त हो गया है। जीवित जीवों के लिए उपलब्ध ताजे पानी का अनुपात काफी कम है, इसलिए इसका उपयोग संयमित तरीके से किया जाना चाहिए और प्रदूषित नहीं होना चाहिए! ग्रह पर हर चौथे व्यक्ति के पास स्वच्छ पेयजल की कमी है। विश्व के कई क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं है।
जलमंडल के विभिन्न घटक अलग-अलग तरीकों से और अलग-अलग गति से जल चक्र में भाग लेते हैं। ग्लेशियरों में पानी के पूर्ण नवीनीकरण में 8000 वर्ष, भूजल - 5000 वर्ष, महासागर - 3000 वर्ष, मिट्टी - 1 वर्ष लगते हैं। वायुमंडलीय वाष्प और नदी का पानी 10-12 दिनों में पूरी तरह से नवीनीकृत हो जाता है। प्रकृति में जल चक्र में लगभग 1 मिलियन वर्ष लगते हैं।
ऑक्सीजन चक्र ऑक्सीजन जीवमंडल में सबसे आम तत्वों का हिस्सा है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। ऑक्सीजन पानी के अणुओं और जीवित जीवों (प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड) का हिस्सा है। ऑक्सीजन का उत्पादन उत्पादकों (हरे पौधों) द्वारा किया जाता है। ओजोन ऑक्सीजन चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओजोन परत समुद्र तल से 20-30 किमी की ऊंचाई पर स्थित है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 2 मुख्य प्रक्रियाओं से प्रभावित होती है: 1) प्रकाश संश्लेषण 2) कार्बनिक पदार्थ का अपघटन, जिसके दौरान इसका उपभोग किया जाता है।
ऑक्सीजन चक्र एक धीमी प्रक्रिया है। वायुमंडल में सारी ऑक्सीजन को पूरी तरह से नवीनीकृत होने में लगभग 2000 वर्ष लगते हैं। तुलना के लिए: वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का पूर्ण नवीकरण लगभग 3 वर्षों में होता है। अधिकांश जीवित जीवों द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग आंतरिक दहन इंजनों में, ताप विद्युत संयंत्रों की भट्टियों में, विमान और रॉकेट इंजनों आदि में ईंधन जलाने पर किया जाता है। अतिरिक्त मानवजनित खपत ऑक्सीजन चक्र के संतुलन को बिगाड़ सकती है। अब तक, जीवमंडल मानव हस्तक्षेप की भरपाई कर रहा है: नुकसान की भरपाई हरे पौधों द्वारा की जाती है। वन क्षेत्र के और कम होने तथा अधिक से अधिक ईंधन जलने से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी।
क्या यह महत्वपूर्ण है!!! जब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 16% तक कम हो जाती है, तो एक व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है (विशेष रूप से हृदय प्रभावित होता है), 7% तक, व्यक्ति चेतना खो देता है, और 3% तक मृत्यु हो जाती है।
कार्बन चक्र
कार्बन चक्र कार्बन कार्बनिक यौगिकों का आधार है; यह प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के रूप में सभी जीवित जीवों का हिस्सा है। कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रवेश करता है। वायुमंडल में, जहां अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड केंद्रित है, एक विनिमय लगातार होता रहता है: पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, और सभी जीव श्वसन के दौरान इसे छोड़ते हैं। सीओ 2 के रूप में 50% तक कार्बन डीकंपोजर - मिट्टी के सूक्ष्मजीवों द्वारा वायुमंडल में वापस आ जाता है। कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में चक्र छोड़ता है।
कार्बन चक्र पर मानव प्रभाव टेक्नोजेनिक मानव गतिविधि कार्बन चक्र के प्राकृतिक संतुलन को बाधित करती है: 1) जैविक ईंधन के दहन के दौरान, लगभग 6 बिलियन टन सीओ 2 सालाना वायुमंडल में उत्सर्जित होता है: ए) थर्मल पावर प्लांटों में बिजली उत्पादन बी ) कार से निकलने वाली गैसें 2) वनों का विनाश। पिछले 100 वर्षों में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगातार और तेजी से बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड + मीथेन + जल वाष्प + ओजोन + नाइट्रोजन ऑक्साइड = ग्रीनहाउस गैस। इसका परिणाम ग्रीनहाउस प्रभाव - ग्लोबल वार्मिंग है, जो बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकता है।
नाइट्रोजन चक्र मुक्त रूप में, नाइट्रोजन वायु का एक घटक है - 78%। नाइट्रोजन जीवों के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। नाइट्रोजन सभी प्रोटीन का हिस्सा है। नाइट्रोजन अणु बहुत मजबूत होता है, यही कारण है कि अधिकांश जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित करने में असमर्थ होते हैं। जीवित जीवों द्वारा नाइट्रोजन को केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ यौगिकों के रूप में अवशोषित किया जाता है। रासायनिक यौगिकों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ज्वालामुखीय और तूफान गतिविधि के परिणामस्वरूप होता है, लेकिन अधिकतर सूक्ष्मजीवों - नाइट्रोजन फिक्सर्स (नाइट्रोजन-फिक्सिंग बैक्टीरिया और नीले-हरे शैवाल) की गतिविधि के परिणामस्वरूप होता है।
नाइट्रोजन पौधों की जड़ों में नाइट्रेट के रूप में प्रवेश करती है, जिसका उपयोग कार्बनिक पदार्थ (प्रोटीन) के संश्लेषण के लिए किया जाता है। पशु पौधों या पशु खाद्य पदार्थों के माध्यम से नाइट्रोजन का उपभोग करते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों के टूटने से नाइट्रोजन वायुमंडल में वापस आ जाती है। मिट्टी के जीवाणु प्रोटीन को अकार्बनिक पदार्थों - गैसों - अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड में विघटित करते हैं, जो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। जल निकायों में प्रवेश करने वाला नाइट्रोजन पौधे-पशु-सूक्ष्मजीव खाद्य श्रृंखला से भी गुजरता है और वायुमंडल में लौट आता है।
नाइट्रोजन चक्र पर मानव प्रभाव टेक्नोजेनिक मानव गतिविधि नाइट्रोजन चक्र के प्राकृतिक संतुलन को बाधित करती है। भूमि की जुताई करते समय, सूक्ष्मजीवों - नाइट्रोजन फिक्सर्स की गतिविधि लगभग 5 गुना कम हो जाती है, इसलिए मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। इसलिए, लोग मिट्टी में अतिरिक्त नाइट्रेट मिलाते हैं, जो खनिज उर्वरकों में शामिल होते हैं। गैस, तेल और कोयले के दहन और प्रसंस्करण के दौरान बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में प्रवेश करती है और अम्लीय वर्षा के रूप में गिरती है। नाइट्रोजन उर्वरकों के उत्पादन को कम करने, वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड के औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने आदि से प्राकृतिक नाइट्रोजन चक्र को बहाल करना संभव है।
फास्फोरस चक्र
पानी, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन चक्रों के विपरीत, जो बंद हैं, फॉस्फोरस चक्र खुला है, क्योंकि फॉस्फोरस वायुमंडल में छोड़े गए वाष्पशील यौगिक नहीं बनाता है। फॉस्फोरस चट्टानों में निहित होता है, जहां से यह चट्टानों के प्राकृतिक विनाश के दौरान या जब फॉस्फोरस उर्वरकों को खेतों में लागू किया जाता है तो पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश करता है। पौधे अकार्बनिक फास्फोरस यौगिकों को अवशोषित करते हैं, और जो जानवर इन पौधों को खाते हैं वे अपने ऊतकों में फास्फोरस जमा करते हैं। जानवरों और पौधों के शवों के अपघटन के बाद, सारा फास्फोरस चक्र में शामिल नहीं होता है। इसका कुछ भाग मिट्टी से बहकर जल निकायों (नदियों, झीलों, समुद्रों) में चला जाता है और नीचे तक बस जाता है। मनुष्यों द्वारा पकड़ी गई मछलियों के साथ फॉस्फोरस थोड़ी मात्रा में भूमि पर लौट आता है।
फास्फोरस चक्र पर मानव प्रभाव मानव प्रभाव के तहत भूमि से समुद्र तक फास्फोरस का स्थानांतरण उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है। जब जंगलों को नष्ट किया जाता है और मिट्टी की जुताई की जाती है, तो सतही जल प्रवाह की मात्रा बढ़ जाती है, और इसके अलावा, खेतों से नदियों और झीलों में लगाए जाने वाले फॉस्फोरस उर्वरक भी प्रवेश कर जाते हैं। चूँकि भूमि पर फॉस्फोरस का भंडार सीमित है, और समुद्र से इसकी वापसी मुश्किल है, भविष्य में कृषि में फॉस्फोरस की कमी हो सकती है, जिससे पैदावार (मुख्य रूप से अनाज की फसलें) में कमी आएगी।